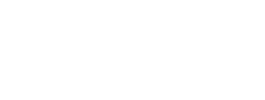यह लेख श्री शेखर पाठक की पुस्तक ‘दास्तान-ए-हिमालय’ भाग 2 के आलेख का सम्पादित रूप है। यह पुस्तक रज़ा फाउण्डेशन और वाणी प्रकाशन द्वारा इसी माह प्रकाशित की जा रही है। शीध्र ही शेखर जी की 1987 में पहली बार प्रकाशित किताब ‘उत्तराखण्ड में कुली बेगार प्रथा’ को नवारुण प्रकाशन द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।
पहाड़ के संपादक व संस्थापक शेखर पाठक प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक हैं। वे कुमाऊँ विश्वविध्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। वे नेहरू मेमोरियल म्यूज़ीयम नई दिल्ली व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला के फ़ेलो भी रहे हैं। पहाड़ों के गहन जानकार उन्होंने पहाड़ों को समझने से लिए कई यात्राएँ की एयर लगभग सभी असकोट आरकोट यात्राओं में भागीदारी की।
बेगार का अभिप्राय
बेगार प्रथा, जो हर सामंती समाज का अंग रही है, औपनिवेशिक काल में भी जारी रही। औपनिवेशिक शासन ने शोषण-उत्पीड़न के अधिकांश सामंती उपकरणों को ज्यों का त्यों अपना लिया था। 1815 ई. में जब औपनिवेशिक शासक कुमाऊं आये तो गोरखा शासन (1790-1815 ई.) की तमाम क्रूरताओं से अवगत होने के बावजूद उन्होंने अपना शासन नये सिरे से आरंभ नहीं किया। हाँ, बाहरी तौर पर, विशेष रूप से दासता को समाप्त करने के संदर्भ में, कुछ उदारता का प्रदर्शन उन्होंने अवश्य किया। किंतु बेगार सहित अनेक प्रचलित प्रथाओं को बनाये रखा। बल्कि कम्पनी सरकार ने बेगार को नियमित शोषण का रूप दिया और बंदोबस्तों में मनमानी धाराएँ डालकर इसे प्रामाणिकता प्रदान की।
बेगार का सामान्य अभिप्राय मजदूरी-रहित जबरन श्रम था। औपनिवेशिक कुमाऊँ में इसका अभिप्राय मजदूरी-रहित या अल्प मजदूरी देकर कराये गये जबरिया श्रम और जबरन सामग्री लिये जाने की प्रक्रिया से था। बेगार देने के लिए स्थानीय काश्तकारों को बंदोबस्ती इकरारनामों के अनुसार बाध्य किया जाता था। ये धाराएँ भूमि बंदोबस्तों में बेगार को पक्का आधार देने हेतु डाली गयी थीं। हर नये बंदोबस्त के साथ यह प्रथा अधिक शोषक और क्रूर रूप लेती चली गयी।
बेगार प्रथा के तीन संघटक थे: कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश। तीनों के लिए कुली बेगार सम्बोधन का ही प्रयोग हुआ। कुली बेगार का अभिप्राय बिना मजदूरी के जबरन श्रम से था। कुली उतार सिर्फ इस संदर्भ में कुली बेगार से भिन्न थी कि इसमें न्यूनतम मजदूरी देय होती थी, जो अधिकतर दी नहीं जाती थी। कुली बर्दायश का अर्थ विभिन्न पड़ावों में साहबों, सैनिकों, शिकारियों, सर्वेयरों और या उनके दलों को दी जानेवाली विभिन्न प्रकार की सामग्री से था। जब बेगार आंदोलन उग्र रूप लेने लगा तो बेगार को उतार प्रथा का गैरकानूनी दुरुप्रयोग कहा जाने लगा था, जब कि वास्तव में बेगार अंत तक स्वतंत्र रूप से जीवित रही।
कुमाऊं का प्रत्येक भूमिवान व्यक्ति बेगार देने या एवज में इसकी व्यवस्था करने के लिए बाध्य होता था। स्थानीय समाज के 85-90 प्रतिशत लोग काश्तकार थे और जनसंख्या का शेष हिस्सा भी सामाजिक-आर्थिक रूप से दयनीय होने के कारण बहुसंख्यक समाज से भिन्न नहीं था। इस प्रकार कुछ ब्राह्मणों, प्रधानों, थोकदारों, भूतपूर्व अधिकारियों या सैनिकों को छोड़कर पूरा कुमाऊँनी समाज बेगारग्रस्त था।
बेगार: स्वरूप् और विकास बेगार-उन्मूलन आंदोलन
बेगार प्रथा कुमाऊँ में औैपनिवेशिक काल में लगभग 105 साल तक (1815 से 1921.) जीवित रही। इस प्रथा के विकास की तीन अवस्थाएं थीं। पहली अवस्था नेपाल युद्ध से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व तक; दूसरी अवस्था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 1885 के आसपास तक; और तीसरी अवस्था तब से 1921 तक रही। पहली अवस्था में प्रचलित बेगार प्रथा प्रारम्भ में उदार और फिर अनुदार नीति से चल कर नियमबद्ध हो गयी। दूसरी में यह अपने शोषक स्वरूप की पराकाष्ठा पर पहुँची और तीसरी में इसके विरूद्ध जन-आंदोलन हुआ। जन-आंदोलनों के प्रभाव से संशोधन और समझौतों का क्रम चला और अंततः इसे पूरी तरह उठाना पड़ा।
बेगार आंदोलन के दो स्पष्ट दौर हैं। पहला प्रारंभ से 1912 तक का है। इसमें हम बिखरे व्यक्तिगत आक्रोशों को असंगठित विरोधों में रूपांतरित होते देखते हैं यह दौर अपेक्षाकृत लम्बा, जागृति की धीमी प्रक्रिया से जुड़़ा और स्थानीय आक्रोशों की अभिव्यक्तियों से भरा है। 1913 के बाद दूसरा दौर चलता है। इसमें संगठित विरोधों ने व्यापक जन-आंदोलन का रूप धारण किया। यह दौर एक दशक से भी कम अवधि का होने के बावजूद अपार सक्रियता, संगठन-प्रक्रिया और पराकाष्ठा पर पहुँचे प्रतिरोध से युक्त है।
1815 ई. में कम्पनी सरकार के कुमाऊं आगमन से 19वीं सदी के अंत तक यहाँ बेगार के विरोध में किसी बड़े जन-आंदोलन के प्रमाण नहीं मिलते। ऐसा भी नहीं कि इस बीच बिल्कुल चुप्पी रही हो, पर लगभग सात दशकों तक छिटपुट व्यक्तिगत प्रतिरोधों/असहमतियों को छोड़कर बेगार के विरोध में कभी सामूहिक प्रतिरोध नहीं हो सका। इस दौर में व्यक्तिगत या ग्रामीण समूह स्तर पर जब भी लोग बेगार-बर्दायश देने नहीं गये, उसके पीछे व्यक्तिगत कार्यों की अधिकता, अभावग्रस्तता या प्रधान-पटवारियों के प्रति आक्रोश की उपस्थिति महत्वपूर्ण कारण रही थी।
1827 में काली कुमाऊँ के जमींदार ने सैनिक बैरकों के निर्माण हेतु पाथर उपलब्ध कराने से इन्कार किया था। 1830 ई. में लोहाघाट में मांग के मुताबिक कुली नहीं आये। 1832 में पिथौरागढ़ में भी यही स्थिति रही। 1837-38 में अलमोड़ा तथा लोहाघाट में सैनिक दलों को रसद (बर्दायश) मिलने में बहुत अधिक कठिनाई उठानी पड़ी।
1841 में लोहाघाट में कम मजदूरी दी जाने के कारण कुलियों ने उसे लेने और काम करने से इन्कार कर दिया। 1844 में सोमेश्वर से अलमोड़ा के बीच पिलग्रिम को पर्याप्त कुली नहीं मिले। सैनिकों के लिए अन्न मांगा जाने लगा तो लोहाघाट के काश्तकारों ने विरोध किया। इसी तरह 1855 में कुली जुटाने में कठिनाई हुई, जो 1857 में और भी बढ़ गई। विद्रोह के समय हेनरी रैमजे ने कैदियों से कुलि कार्य कराया। लेकिन ये किसी व्यापक आंदोलन के हिस्से नहीं थे। ये संदर्भ जनसामान्य की बेगार के प्रति अरुचि को उजागर करते हैं।
बेगार के विरोध में कदाचित 1860 के बाद भी वातावरण नहीं बन सका। ग्रामीण काश्तकार बेगार के प्रति अपनी अरूचि का प्रदर्शन तरह-तरह से करते रहे, पर सामूहिक स्वरूप धारण न कर सकने के कारण यह प्रभावशाली न हो सका। 1868 ई. से पूर्व उत्तराखण्ड में न देशी भाषा का कोई स्थानीय पत्र था और न कोई स्थानीय संगठन। पत्रों का प्रारम्भिक रूप भी सरकारपरस्त अधिक था, लेकिन सरकार के विरोध के उद्देश्य से न सही, बेगार सम्बंधी कुछ समाचार इन पत्रों में आने लगे। चूंकि उस समय ग्रामीण क्षेत्रों की घटनाओं का समाचार पत्रों तक पहुंचना सम्भव नहीं हुआ था, अतः इन प्रसंगों के अवर्णित रह जाने की सम्भावना है।
अलमोड़ा में 1871 से ‘अलमोड़ा अखबार’ और इससे पूर्व 1868 में नैनीताल से ‘समय विनोद’ के प्रकाशन और मिशन स्कूलों की शिक्षा के प्रसार के साथ यहां एक नरमपंथी चेतना फैलने लगी। 30 साल बाद 1901 में देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना,1902 से ‘गढ़वाल समाचार’ और 1905 से ‘गढ़वाली’ के प्रकाशन के साथ यह चेतना तेजी से उत्तराखण्ड स्तर तक फैलती चली गयी। यह चेतना बेगार-उन्मूलन या विरोध का स्पष्ट लक्ष्य स्वीकार नहीं कर सकी।
1893 से बेगार-सम्बंधी प्रश्न काउंसिलों में उठने लगे। प्रांतीय काउंसिल में 1893 में बर्दायश रसद, 1894 में बेगार-सम्बंधी तथा 1897 में विशेष रूप से कुमाऊं में बेगार की स्थिति-सम्बंधी और गर्वनर जनरल की काउंसिल में 1893 में ही बेगार-बर्दायश-सम्बंधी प्रश्न पूछे गये थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के अधिवेशन में प्रयासों के बावजूद बेगार-सम्बंधी प्रश्न नहीं उठ सका, पर उसके 1893 के अधिवेशन में बेगार के विरोध में प्रस्ताव पारित हो गया। उसका असर पौ (1892-96 ई.) के बंदोबस्त पर पड़ा और उसने बेगार के सम्बंध में इसी दबाव के कारण अपने को अन्य औपनिवेशिक अधिकारियों से कुछ उदार प्रमाणित करने की कोशिश की। तब बनिया नाली की व्यवस्था आरम्भ हुई। इससे बर्दायश का आतंक कुछ कम हुआ।
1903 में बेगार आंदोलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, यह घटना अलमोड़ा शहर से जुड़े खत्याड़ी गांव के ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से बेगार में जाने से इनकार कर दिये जाने की थी। यद्यपि इस घटना से जितना सम्बंध उक्त नरमपंथी शहरी चेतना का था उससे अधिक ग्रामीण काश्तकारों पर बेगार के दबाव के निरंतर बढ़ते जाने का था। रैमजे के काल में हुई सोमेश्वर की घटना, जिसमें काश्तकारों ने बेगार देने को आने से इनकार किया था, के बाद यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। पर दोनों में महत्वपूर्ण अंतर था। सोमेश्वर के सामूहिक प्रतिरोध को रैमजे ने जुर्माना लगा कर कुचल दिया था और इसके बाद ग्रामीण समुदाय न प्रतिरोध कर सका और न ही न्यायालय की शरण में जा सका। जबकि खत्याड़ी की घटना के बाद प्रतिरोधों का क्रमबद्ध सिलसिला चला और और ये ग्रामीण सरकार की बेगार नीति के विरूद्ध उच्च न्यायालय का निर्णय लाने में सफल रहे। जुलाई 1903 ई. खत्याड़ी के 16 ग्रामीण बेगार देने हेतु तहसील में बुलाये गये। मना करने पर उनसे कारण पूछा गया और उत्तर हेतु उपस्थिति अनिवार्य बताई गई। ग्रामीणों ने इस आदेश को भी नहीं माना। मुकदमा चला और 16 में से 14 को प्रति व्यक्ति दो रुपये जुर्माना अथवा सामान्य कैद की सजा हुई। इस निर्णय के विरूद्ध गोपिया तथा साथियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की और न्यायालय ने सभी आरोपों को रद्द कर उन्हें मुक्त कर दिया। इस निर्णय के बाद भी सरकार ने काउंसिल में बेगार के जारी रहने के पक्ष में कानून पारित करवाने का प्रयत्न किया, लेकिन गवर्नर जनरल ने इसकी स्वीकृति नहीं दी।
1903 में जब लॉर्ड कर्जन अलमोड़ा से गढ़वाल गये तो गिवाड़ के गौरीदत्त बिष्ट तथा टोटाशिलंग के महंत नारायण दास ने कुली बेगार और जंगलात की समस्याओं के सम्बंध में कर्जन को आवेदन दिया था। ग्रामीणों ने इससे पहले भी अनेक प्रार्थनापत्रों में कुली उतार और जंगलात की समस्याएँ सुलझाने का निवेदन किया था। 1905 के बाद शहरी भद्रजनों ने बेगार के विरोध या इसके स्वरूप में संशोधनों हेतु नियमबद्ध उदार आंदोलन प्रारम्भ किया। 1907 में अलमोड़ा में बेगार-विरोधी सभा हुई। डिप्टी कमिश्नर के पास जानेवाले शिष्टमंडल के एक सदस्य हरिराम पांडे ने 1806 से 1907 तक के कुली-बर्दायश कानूनों की आलोचना करते हुए बताया कि यह न सिर्फ नियम-विरूद्ध कार्य है, वरन् अत्याचार भी है।
पत्र-पत्रिकाओं में भी इस सम्बंध में अनेक लेख प्रकाशित हुए। श्रीनगर (गढ़वाल) के निवासियों ने भी डिप्टी कमिश्नर को इस सम्बंध में एक प्रार्थनापत्र दिया। इस शिष्टमंडल ने, जिसमें गिरिजादत्त नैथाणी भी थे, स्थायी कुलियों की व्यवस्था करने की माँग की और “बेगार बर्दास्या भाइयों की अपील” नाम से एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर गांव-गांव भेजी। लेकिन 1908 में बरेली में हुए कुमाऊँ तथा रूहेलखण्ड दरबार में प्रांतीय लाट हिवेट ने कुली बेगार की शोषक प्रथा में परिवर्तन करना असम्भव बताया।
1909 के प्रारम्भ में ‘मॉडर्न रिव्यू’ ने बेगार पर एक सशक्त लेख प्रकाशित किया। अलमोड़ा अखबार तथा गढ़वाली के अलावा अन्य पत्रों ने भी बेगार-सम्बंधी लेख प्रकाशित किये। लेकिन यह जागरण कुछ पढ़े-लिखे और शहरी लोगों तक और प्रत्यक्ष प्रतिरोध के रूप में सिर्फ गांवों तक सीमित रहा। शहरी नेतृत्व नहीं समझ सका कि बेगार आंदोलन की वास्तविक ताकत कुमाऊं के काश्तकार है और सर्वाधित बेगारग्रस्त होने के कारण बिना उनकी हिस्सेदारी के आंदोलन की सफलता संदिग्ध रहेगी।
इस प्रकार 1815 से 1912 तक के 97 सालों में पहले छिटपुट, फिर सामूहिक पर असंगठित और अंततः एक उदार आंदोलन के स्तर पर बेगार का विरोध हुआ। इस सदी के प्रारम्भ में जब बेगार के प्रति असंतोष अधिक तेजी से बढ़ने लगा तो बेगार में संशोधन करके उसे किसी तरह जीवित रखने के उपाय किये जाने लगे। बचाव के रास्ते के रूप में एजेंसियां बनायी गयीं और इन्हें सरकार का पर्याप्त सहयोग मिला। इस तरह कुली एजेंसियां बेगार आंदोलन के पहले दौर का एक बड़ा परिणाम थीं।
बेगार-उन्मूलन आंदोलनः दूसरा दौर
1913 से पूर्व बेगार में सिर्फ संशोधन चाहने वाला उदार आंदोलन 1913 से 1916 के बीच बेगार के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हुआ। इन्हीं सालों की सामाजिक-राजनैतिक हलचलों और औपनिवेशिक दमन के पूर्ववत रहने के कारण कुमाऊं की समस्याओं को हल करने हेतु स्थानीय संगठन की जरूरत से महसूस की गयी। 1916 जहाँ कांग्रेस की दो धाराओं में एका होने का साल था, वहीं कुमाऊँ में इस साल एक क्षेत्रीय सामाजिक-राजनैतिक संगठन कुमाऊँ परिषद का जन्म हुआ। इस संगठन ने उत्तराखण्ड स्तर पर इतनी जागृति पैदा की कि 1920 के अंत तक कुमाऊँ प्रत्यक्ष आंदोलन के कगार पर था।
तीसरे और अंतिम चरण (1920 के बाद) का प्रारम्भ कुमाऊँ परिषद् के काशीपुर अधिवेशन से हुआ। जिसमें सरकार को तुरंत बेगार उठाने की चेतावनी दी गयी और ऐसा न होने पर बेगार न देने का आह्वान किया गया। अंततः 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर (अलमोड़ा) में जनता ने बेगार-उन्मूलन की घोषणा की और प्रत्यक्ष रूप से उतार न देने की कार्यवाही की।
अप्रैल 1913 में अलमोड़ा शहर से जुड़े गांवों में उतार लगने की घोषणा हुई और इस घटना के साथ आंदोलन का दूसरा दौर आरम्भ हुआ, पर इस समय तक आंदोलनकारियों की अस्पष्ट सोच में कोई परिवर्तन या प्रखरता नहीं आयी थी।
अगस्त 1913 में अलमोड़ा के 10 गाँवों-मुहल्लों के लोगों का शिष्टमंडल कमिश्नर के पास गया। शिष्टमंडल के प्रमुख बद्रीदत्त जोशी ने कमिश्नर से वाद-विवाद में कहा कि यह आदेश नियम-विरूद्ध है। किसी भी मनुष्य को उसकी इच्छा के विरूद्ध बोझ ले जाने को विवश करना दंडसंहिता की धारा-374 के अनुसार दंडनीय है। इन तर्कों से अप्रभावित कमिश्नर का कहना था कि कुमाऊँ से बेगार उठाना असंभव है। उसने इसे उठाने की प्रार्थना की तुलना चांद माँगने की प्रार्थना से की थी। पर विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के कारण न सरकार ने कोई कदम उठाया न अलमोड़ावासियों ने उतार दी और न ही आंदोलन आगे बढ़ पाया।
सदी के प्रारम्भ से ही जिस तरह की सामाजिक-राजनैतिक शक्तियों की रचना हो रही थी और औपनिवेशिक व्यवहार बदल नहीं रहा था, उसमें एक क्षेत्रीय संगठन की सम्भावना स्वाभाविक थी। 1916 में कुमाऊँ परिषद् का जन्म कहीं न कहीं 1870 के आसपास से प्रारम्भ सुधारवादी समझौतापरस्त चेतना के प्रौढ़ और सोद्देश्य होने से जुड़ा था। इस चेतना के विकसित होने के बावजूद यह संस्था बुनियादी रूप से भिन्न थी। यद्यपि प्रारम्भ में यह परिषद एक शहरी संगठन थी, पर धीरे-धीरे इसका प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होता गया।
गाँव में परिषद के संगठन के साथ ही स्वतंत्र रूप से परिषद से अप्रभावित जन-प्रतिरोध भी चलते रहे। नवम्बर 1917 में बीरोंखाल में बर्दायश देरी से लाने वाले मालगुजार से जब चपरासी ने मारपीट की तो ग्रामीणों ने इसे सहन नहीं किया और चपरासी को पीट डाला। बेरीनाग में स्थानीय काश्तकारों ने अप्रैल 1918 में बेरीनाग से थल तक तहसीलदार का बोझ ले जाने से इनकार कर दिया। मई तथा अक्टूबर 1918 में चमोली तथा गंगोली में भी इसी तरह के प्रतिरोध हुए।
इस बीच मार्च 1918 में अपने अंतिम सालों में अपनी प्रखरता और स्पष्टता के चलते बेगार-विरोधी वातावरण बनाने के आरोप में 48 साल से चल रहे अलमोड़ा अखबार को बंद कर देना पड़ा। लेकिन यह सक्रियता नहीं रोकी जा सकी और अक्टूबर 1918 से ‘शक्ति’ का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसने बेगार आंदोलन के दूसरे दौर के अंतिम ढाई सालों में आसाधारण योगदान दिया।
दिसम्बर 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में सम्पन्न परिषद के दूसरे अधिवेशन में भी मतभेद बना रहा। पर अंततः हरगोविंद पंत का वह प्रस्ताव पारित हो गया जिसमें दो साल के भीतर बेगार उठाने की माँग की गयी थी। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी गयी कि दो साल के भीतर उतार न उठाने पर जनता खुद सत्याग्रह करेगी। इस साल बद्रीदत्त पांडे गांधी से मिलने कलकत्ता गये। गांधी ने व्यस्तता के कारण कुमाऊं आने में असमर्थता व्यक्त की।
मार्च 1919 में श्रीनगर में गढ़वाल परिषद की सभा में राजभक्ति और बेगार-विरोधी प्रस्ताव साथ-साथ पारित हुए। इसी माह के अंत में विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत के उत्सव में तारादत्त गैरोला ने बेगार को शानदार अंग्रेजी राज के लिए कलंक के समान बताया। मई 1919 में नंदा देवी तथा बनाड़ी देवी में हुई जनसभाओं में भी बेगार-विरोधी प्रस्ताव पारित हुए। जून 1919 में पटवारी को दिये जानेवाले खाजे (अन्न) को रोकने की घोषणा करनेवाले कत्यूर के काश्तकार तथा मालगुजार अब आंदोलन की चेतावनी भी देने लगे थे।
अक्टूबर 1919 में कुमाऊँ परिषद की मझेड़ा शाखा तथा सहारनपुर में हुई संयुक्त प्रांतीय सभा की 13वीं सालाना बैठक में बेगार-विरोधी प्रस्ताव पारित हुए। इस बीच कमिश्नर विंढम ने बोर्ड ऑफ कम्यूनिकेशंस की उपसमिति की रपट जारी की। इसमें उतार और बर्दायश को नियमबद्ध करके संशोधन का भ्रम पैदा किया गया था। व्यक्तिगत रूप से विंढम को बेगार-विरोधी बताया जाता है, पर इस रपट में संशोधन की गंध के बावजूद उतार और बर्दायश को बनाये रखने का हठ मुख्य था।
कुमाऊँ परिषद का तीसरा अधिवेशन बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में दिसम्बर 1919 में कोटद्वार में सम्पन्न हुआ। जोशी ने जंगलात और बेगार के कष्टों को उच्च श्रेणी के लोगों के आत्मसम्मान की जड़ पर कुठाराघात तो बताया ही, साथ ही यह भी कहा कि इससे गरीबों को भी दुख सहने पड़ते व्यापक आंदोलन की जगह संशोधनों या सरकार की कृपा की चाह बनी रही।
अमृतसर काँग्रेस से लौटने के बाद कुमाऊँ परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाँवों में संगठन कार्य और सभाएँ की तथा परिषद को गाँव-गाँव तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य आरम्भ हुआ। लक्ष्मीदत्त शास्त्री, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, मोहनसिंह मेहता, मथुरादत्त त्रिवेदी आदि ने कितने ही स्थानों पर परिषद की शाखाएँ खोलीं, कुली एजेंसी का विरोध किया और बेगार के विरुद्ध संगठित होंने का आह्वान किया।
सितम्बर 1920 में अलमोड़ा जिला की पट्टी कैरारों के सूर्ना गाँव के लोगों ने कुली व्यवस्था करने तथा तलवाना (जुर्माना) देने से इनकार किया। स्थानीय प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 1920 की मुरादाबाद की संयुक्त प्रांतीय राजनैतिक सभा में भी बेगार उठा लेने का प्रस्ताव पारित कराया। इसके तुरंत बाद मुकंदीलाल तथा हरगोविंद पंत ने अपने ‘शक्ति’ में प्रकाशित लेखों के द्वारा जनता का आह्वान किया कि वे बेगार-बर्दायश लेने से साफ इनकार कर दें। नवम्बर 1920 में गढ़वाल परिषद के कोटद्वार में सम्पन्न पहले अधिवेशन में जनता को यह बताने का निर्णय हुआ कि बेगार देना कानून के खिलाफ है, अतः बेगार देने से पूरी तरह इनकार करें। 1920 में पूरे संयुक्त प्रांत में बेगार-विरोधी आंदोलन चल रहा था।
कुमाऊँ परिषद का चौथा अधिवेशन दिसम्बर 1920 में काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ। यह बिना रायबहादुरों की अध्यक्षता का पहला अधिवेशन था और पिछले तीन अधिवेशनों से भिन्न था। साथ ही इस पर असहयोग आंदोलन का असर भी था। हरगोविंद पंत इस समय प्रगतिवादियों के प्रतिनिधि और प्रतीक थे। वे न सिर्फ कुली उतार को समाप्त करना, वरन् इस माध्यम से असहयोग में भी शामिल होना चाहते थे। नरमपंथियों और सरकारपरस्तों के अनेक प्रयत्नों के बावजूद इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। कुमाऊँ के तमाम प्रतिनिधियों ने खड़े होकर यह प्रतिज्ञा की कि वे अब कुली उतार नहीं देगें और इस कलंक को हटा कर रहेंगे। सरकारपरस्तों ने प्रगतिवादियों के निर्णय को बदलने का पूरा प्रयास किया, पर अंत में अपनी पराजय के साथ उन्हें सभास्थल भी छोड़ना पड़ा।
शहरी नेता नागपुर से अभी लौट ही रहे थे कि ग्रामीणों की सबसे बड़ी बेगार-विरोधी अभिव्यक्ति 1 जनवरी 1921 को चामी (कत्यूर) के हरू मंदिर की सभा में हुई। इसमें कत्यूर के 400 से अधिक लोग उपस्थित थे। स्थानीय पटवारी ने इस सभा के बाबत रपट भेजी थी। इस सभा में उतार न देने की तथा बागेश्वर में उपस्थित होकर कुमाऊँ के जनसामान्य तक यह निर्णय पहुँचाने की शपथ ली गयी। शक्ति में भी बागेश्वर आने का और बेगार उठा देने का आह्वान किया गया था। इस समय कुमाऊँ का सामाजिक-राजनैतिक तापमान अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था। गाँवों में, विशेष रूप से कत्यूर क्षेत्र के, बेगार-विरोधी लहरें पूरी तरह फैल चुकी थीं और उत्तरायणी के मेले में इस सबकी सम्मिलित अभिव्यक्ति होने का सभी को इंतजार था।
जनवरी 1921 के पहले सप्ताह में द्वाराहाट तथा गणाई में जंगलात के बड़े अधिकारियों को कुली नहीं मिल पाये। यह काशीपुर के निर्णय का असर तो था ही, साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध के कारण भी था।
10 जनवरी 1921 को हरगोविंद पंत, चिरंजीलाल, बद्रीदत्त पांडे, चेतराम सहित लगभग 50 कार्यकर्ता अलमोड़ा से बागेश्वर पहुँचे, जहाँ शिवदत्त पांडे, रामदत्त और मोहनसिंह मेहता सहित दर्जनों ग्रामीण कार्यकर्ता तैयारी किये हुए थे। कत्यूर घाटी और बागेश्वर में पहली बार ‘भारत माता की जय’, ‘महात्मा गांधी की जय’ तथा ‘वन्देमातरम’” के नारे गूंजे। कुछ आंदोलनकारियों ने नागपुर से लायी गयी खद्दर की टोपियाँ पहन रखीं थीं। 12 जनवरी को ‘कुली उतार बंद करो’ लिखा हुआ बैनर जुलूस के साथ बाजारों में घुमाया गया। पहली बार उत्तरायणी मेले में इस तरह का दृश्य सामने आ रहा था। अंत में सरयू तट पर यह जुलूस एक विशाल जनसभा में बदल गया। इस सभा में 10 हजार से अधिक लोग थे। सभा में उतार न देने की शपथ ली गयी। इसी दिन सिलौट महादेव (गढ़वाल) में ईश्वरीदत्त ध्यानी के प्रयत्नों से एक विशाल जनसभा हुई और उतार न देने का निर्णय लिया गया।
13 जनवरी के दिन दोपहर एक बजे के आसपास सरयू के किनारे एक विशाल सभा हुई। औपनिवेशिक शासन और नीतियों की आलोचना करते हुए देश तथा कुमाऊँ की वर्तमान परिस्थितियाँ जनता के सामने रखी गयी। सभी ने बेगार न देने की शपथ ली। इनमें अनेक मालगुजार भी सम्मिलित थे, जिन्होंने कुली रजिस्टरों को सरयू में प्रवाहित कर दिया और यह संदेश देकर अपने गाँवों को आदमी भेजे कि उतार न दें।
14 जनवरी 1921 को डिप्टी कमिश्नर डायबिल को पता चला कि जनता पर बहुत गम्भीर प्रभाव हुआ है; बागेश्वर की मुख्य पट्टियों के मालगुजारों-थोकदारों पर अब प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और उन्होंने आदेश मानने तथा कुली उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। डायबिल ने आंदोलनकारियों को डांट-डपट कर डराने की कोशिश की और बागेश्वर छोड़ने का भी आदेश दिया, पर जनता की सक्रियता ने न नेताओं को डरने दिया, न ही बागेश्वर से वापस जाने दिया। 16 जनवरी को, जब मेला सिमटने लगा था, मुख्य आंदोलनकारी बागेश्वर से अलग-अलग इलाकों को गये ताकि बागेश्वर का निर्णय सभी तक पहुँचाया और निश्चय पर कायम रहने का आह्वान किया जा सके।
बागेश्वर की सफलता के बाद वहां लिये गये निर्णय और उसके प्रभाव को कुमाऊं के हर अंचल की जनता तक पहुँचाने की सर्वाधिक आवश्यकता थी। इसके लिए आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव जाकर जनता को, जो हुआ उसे बताने और जो किया जाना है उसे समझाने का कार्य शुरू किया। यह कार्य इतने नियोजित तथा प्रभावशाली ढंग से किया गया कि बागेश्वर और आसपास की चार पट्टियों में फैला आंदोलन सम्पूर्ण कुमाऊँ में फैल गया।
18 जनवरी 1921 के बाद कुमाऊँ के किसी न किसी इलाके में रोज सभा होती रही और जनता के उत्साह और हिस्सेदारी का तापमान कभी भी नीचे नहीं आ सका। इस बीच अलमोड़ा, चमेठाखाल, डंगोली, पिथौरागढ़, लोहाघाट, रामनगर, कपकोट, बिसाड़, कंडिया महादेव, जमकेश्वर, सालम, देवाल तथा बंदखणी आदि प्रमुख स्थानों सहित सैकड़ों गाँवों में जनसभाएँ हुई।
यद्यपि 17 जनवरी 1921 को ही डायबिल मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर वह ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने आंदोलनकारी तथा शांत पहाड़ी काश्तकारों के आक्रोश तथा उत्तेजना को असाधारण स्थिति पर पहुँचा पाया था। फिर भी वह चाहते थे कि मुख्य नेताओं, जिद्दी थोकदारों-मालगुजारों तथा छोटे स्थानीय आंदोलनकारियों का दमन किया जाना चाहिए। सभा करने से आंदोलन के और जोर पकड़ने की संभावना थी।
भयग्रस्तता की इस स्थिति में उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट को तैयार रहने को लिखा था। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आंदोलन में शामिल होने से डायबिल की चिंता स्वाभाविक रूप से अधिक बढ़ गयी थी। वह आंदोलन को तोड़ने हेतु प्रलोभनों का प्रयोग करने लगे। सरकारपरस्त मालगुजार नियुक्त करने या उनके पारिवारिक जनों को पद प्रतिष्ठा देने पर भी विचार किया गया। फरवरी 1921 से ही प्रशासन ने आंदोलन को दबाने और कमजोर करने की पूरी कोशिश की, किंतु उसे इसी अनुपात में जन-प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। कुली देने से इनकार करने पर जमीन छीन जाने के आदेश दिये जाने के बावजूद कुली न मिले। तहसीलदारों, डिप्टी इंस्पेक्टरों की भी यही स्थिति रही। रानीखेत में आंदोलन को तोड़ने हेतु विंढम ने डायबिल के पास एक राजपूत पेशकार तथा एक तहसीलदार भेजा, ताकि राजपूत बहुल क्षेत्र में वे सरकार के पक्ष में कार्य कर सकें, पर वे कुछ नहीं कर सके। मार्च 1921 में आंदोलन अलमोड़ा तथा नैनीताल जिलों में गम्भीर रूप लेने के बाद गढ़वाल जिले में भी फैल गया। जब स्थिति सुधरने की आशा न रही तो दमन शुरू हो गया।
अलमोड़ा जिले में देवालयों के अलावा कहीं भी बिना आज्ञा सभा करने की मनाही थी। सरकार ने एक ओर घोड़ों, खच्चरों तथा कुली एजेंसी की व्यवस्था की घोषणा की, दूसरी ओर मार्च 1921 के तीसरे सप्ताह में कत्यूर को आंदोलित करनेवाले मोहनसिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च को अपनी इच्छा के विरुद्ध वे जमानत पर छूटे। राधाबल्लभ कुली जमादार को कुलियों को भड़काने के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया। रामनगर में अनेक लोगों की बंदूकों के लाइसेंस जब्त किये गये और काश्तकार बेदखल किये गये।
अप्रैल 1921 में गढ़वाल में आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर पहंुच चुका था। ऊपरी गढ़वाल में अनुसूयाप्रसाद बहुगुणा तथा दक्षिणी गढ़वाल में केशरसिंह रावत के नेतृत्व में निरंतर सक्रियता बनी रही। प्रत्यक्ष प्रतिरोध के अनेक उदाहरण मिलते हैं। डिप्टी कमिश्नर मैसन तक को उतार के कुली नहीं मिले। इस कारण गढ़वाल में अनेक मालगुजार बेदखल किये गये और अनेक ग्रामीणों तथा आंदोलनकारियों की बंदूकें भी जब्त हुईं। पिथौरागढ़ में प्रयाग दत्त पन्त तथा कृष्णानन्द उप्रेती ने सधन प्रचार-प्रसार कर कांग्रेस संगठन को भी विकसित किया। प्रयाग दत्त पन्त बागेश्वर से आन्दोलन की उर्जा साथ लेकर वापस अपने इलाके में आये थे।
मई 1921 के दूसरे सप्ताह में शक्ति से, 2 नवम्बर 1920 से 5 अप्रैल 1921 तक के 14 अंकों के 53 लेखों के लिए, 6 हजार रुपये की जमानत मांगी गयी। मई-जून में यह आंदोलन सामान्य बेगार-विरोधी आंदोलन न रह कर राष्ट्रीय असहयोग का हिस्सा बन गया। जून 1921 के बाद भी प्रतिरोध और दमन का क्रम निरंतर चलता रहा। दिसम्बर 1921 में व्यापक गिरफ्तारियां हुईं, जो 1922 ई. के मध्य तक चलती रहीं।
मूल्यांकन
बेगार-उन्मूलन आंदोलन कुमाऊँ का सर्वप्रथम और अब तक शायद अंतिम आंदोलन था जिसमें स्थानीय समाज के विभिन्न वर्गों की अधिकतम हिस्सेदारी रही। सामान्य बेगार-विरोधी व्यक्तिगत आक्रोशों से प्रारम्भ होकर इस प्रक्रिया के संगठित आंदोलन में रूपांतरित होने तक एक स्वाभाविक विकास क्रम देखा जा सकता है।
बेगार आंदोलन का पहला दौर राष्ट्रीय संग्राम के उन वर्षों में पड़ता है जब कांग्रेस में सुधारवादी/नरमपंथी सोच का अधिक प्रभाव था। निवेदनों से संक्षिप्त सुधार हासिल करना इस समय राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर अभीष्ट था। पहला दौर अधिक लम्बा तथा कम सक्रिय और दूसरा दौर एक दशक से कम अवधि का होकर भी बहुत अधिक सघन, संगठित और जनमुखी रहा।
कुमाऊँ परिषद के जन्म के बाद दूसरा हिस्सा सबल होता गया और शहरी आंदोलन की इस धारा तथा भिन्न प्रकार के ग्रामीण आंदोलनों में एका प्रारम्भ हुआ। ग्रामीणों में से उभरे कार्यकर्ता अधिक साहसी तथा नेतृत्व को प्रेरित करनेवाले निकले। ग्रामीण काश्तकारों की ओर से आंदोलन में व्यापक हिस्सेदारी, निर्णय ले सकने और अपने निर्णय पर अटल रहने की आशा के कारण अपनी पराकाष्ठा के समय यह आंदोलन फिर गांवों की ओर उन्मुख हुआ।
आंदोलन में ग्रामीण-शहरी, सयाण-थोकदार, भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी, सैनिक, शिक्षक, छात्र तथा सभी तरह के काश्तकार सम्मिलित हुए। यह व्यापक जन-हिस्सेदारी सिर्फ कुमाऊं परिषद की सभाओं, अलमोड़ा या बागेश्वर तक सीमित न थी, वरन् तराई से भोट और सोर (पिथौरागढ़) से चमेठाखाल (पौड़ी) तक यही प्रक्रिया अभिव्यक्त हुई। आंदोलन में हिस्सेदारी निरंतर बढ़ती गयी।
1920-21 में आंदोलन इतना जनमुखी हो चुका था कि अनेक मालगुजार खुलकर आंदोलन के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। कोई सरकार-समर्थक भी बने रहे तो उनके भाई-भतीजे उनके नियंत्रण से बाहर हो कर स्थानीय नेतृत्व कर रहे थे। हिंसा की सम्भावना या हिंसा में रूपांतरित होने वाली उत्तेजना की उपस्थिति न मान कर भी प्रशासन ने यह स्वीकार किया था कि अनपढ़ आंदोलनकारी अपने नेताओं की अपेक्षा आंदोलन को अधिक आगे ले जायेंगे, क्योंकि गुप्त सूचनाओं के अनुसार उन्हें ज्ञात था कि जहां हरगोविंद पंत सहित सभी नेता उतार आदि की ही निंदा कर रहे थे, वहीं ग्रामीण कार्यकर्ता काश्तकारों से खुशखरीद कुली तक न बनने का वायदा ले रहे थे।
इस प्रकार 1920-21 में बेगार आंदोलन व्यक्तिगत आक्रोशों से असंगठित विरोधों और संगठित विरोधों से व्यापक जन-आंदोलन में रूपान्तरण की प्रक्रिया पूरी कर चुका था। आंदोलन का संचालन पूरी तरह सामूहिक था।
बेगार आंदोलन नेतृत्व के स्वरूप के अनुसार पिरामिडीय (ऊपर एक मुख्य नेता, फिर नेतृत्व की दो-तीन परतें और फिर जनता) नहीं था, वरन् इसमें शिखर का सामूहिक नेतृत्व पूरी तरह से उस बड़े कार्यकर्ता वर्ग तथा ग्रामीण नेतृत्व पर निर्भर रहा, जिसका सीधा सम्बंध स्थानीय जनता से था। नेतृत्व के आत्मविश्वासी होने का मूल कारण ग्रामीणों के बीच व्याप्त जागृति थी।
बेगार आंदोलन की सफलता उन सालों में प्राप्त की गयी थी जब गांधी ने असहयोग आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया था और खिलाफत आंदोलन भी एक प्रकार से असफल हो कर रह गया था। इसलिए इस आंदोलन ने प्रांतीय सरकार को तो प्रभावित किया ही था, एक शोषक-उत्पीड़क प्रथा के अंत से स्थानीय समाज में वह आत्मविश्वास और भी अधिक गहरा और व्यापक हुआ जो आंदोलन के दौर में विकसित हो रहा था। समाज के विभिन्न हिस्सों में जागरण और आत्मसम्मान की असाधारण लहर आयी और औपनिवेशिक शासन के प्रति जितनी अधिक घृणा उत्पन्न हुई उतनी ही आजादी की चाह बढ़ती गयी। स्वयं अलमोड़ा के डिप्टी कमिश्नर डायबिल ने इस आंदोलन के कार्यक्रम और उद्देश्यों को ‘क्रांतिकारी’ और ‘कर्मचारियों के प्रति घृणा भरनेवाला’ तथा ‘सरकारी प्रभुत्व को उखाड़नेवाला’ कहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में ‘स्वराज्य’ की बात सामान्य हो गयी थी।
इस आंदोलन की कुछ कमजोरियों को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। ये कमजोरियां वास्तव में कुमाऊं की 18वीं-19वीं सदियों की सामाजिक रूप से असंतुलित जागृति का परिणाम थीं। आंदोलन पर सवर्णों और विशेष रूप से ब्राह्मणों का नियंत्रण था। यह वर्ग औपनिवेशिक शासन के लाभ भी पूरी तरह प्राप्त करता रहा था।
इस आंदोलन के दौरान विकसित जनचेतना बाद के काल में पूरी तहर अक्षुण्ण नहीं रह सकी और न ही संगठित जनशक्ति का संचय किया जा सका। इसके बाद आजादी के पहले और बाद के सालों में उत्तराखण्ड के जनजीवन में आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर किसी अहम प्रश्न को लेकर कुमाऊं में कोई भी जन-आंदोलन इतना व्यापक, आक्रामक तथा जनता से जुड़ा हुआ देखने में नहीं आया। चिपको आंदोलन तथा नशे के विरुद्ध हुए आंदोलन के बाद उत्तराखण्ड आन्दोलन इसके अपवाद माने जा सकते हैं। पर ये आंदोलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी जारी हैं, अतः अभी इनका समग्र रूप और प्रभाव जानना सम्भव नहीं है।

पहाड़ ऑनलाइन का सम्पादन, पहाड़ से जुड़े सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह करता है। इस उद्देश्य के साथ कि पहाड़ संबंधी विमर्शों को हम कुछ ठोस रूप भी दे सकें।