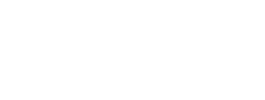इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा का जन्म 10 जनवरी, 1938 को हुआ था और 16 मई, 2021 को देहरादून में उनका निधन हो गया। उनके व्यक्तित्व को अगर एक शब्द में बयान करना हो तो मैं उसे ‘मुस्कुराहट’ का नाम देना चाहूँगा। उनकी यह मुस्कुराहट वाममार्गी मानवता भी थी और उससे आगे समस्त जीव प्रजातियों की बुनियादी एकता पर ठहरकर नज़र डालना भी। चौरासी साल की उम्र में भी वे पदार्थवादी थे, पर एक स्वाभाविक मासूमियत से भरे हुए।
शम्भु नाथ और राजदेई के बेटे
गोरखपुर के शम्भु नाथ और बस्ती में मायके वाली राज देई के बेटे के रूप में लाल बहादुर छपरा, बिहार में पैदा हुए थे। उनके पिता की ओवरसियरी तब वहाँ थी। ननिहाल में संग्रामी और जनप्रतिनिधियों का सिलसिला लगा रहता था। आम भारतीयों की तरह लाल बहादुर भी अपने घोषित जन्मदिन को पैदा नहीं हुए होंगे, ऐसा वे मानते थे। पर हम उन्हें मूलतः गोरखपुर का ही पूत कहेंगे, जिसके लिए वह पश्चिम से वापस आए। वहाँ वाप स आने का रिवाज ही नहीं था। ऊपर से पेरिस के उनके गुरु का उन पर वरदहस्त था।
इस दम्पती के कुल 5 पुत्रियाँ औैर फिर 6 पुत्र जन्मे। बहिनों में तीन पर भाइयों में सिर्फ़ लाल बहादुर बचे। एक ही लाड़ले होने के कारण उनको बहुत तरह से ‘बीमित’ और सीमित किया गया, जिनमें उनकी नाक को छेदना या फ्रॉक पहनाना भी शामिल है। गोरखपुर के बाद कुछ साल क़रीब के क़स्बे आनन्दनगर में पिता के साथ गए। वहाँ की यादें उनको आजन्म आती रहीं। गन्ना मिल परिसर, बँगले तथा मिल की ख़ुशबू उसके मन में बनी रही।
15 अगस्त, 1947 के बाद
यह 1947 का दौर था। यहीं स्कूल में प्रवेश और उसके बाद पहले 15 अगस्त का रोमांचक अनुभव। पहला इनाम। क़स्बाई जीवन के सब अनुभवों से होकर वे गुज़रे। उनको भी अपने शुरुआती शिक्षक बहुत याद रहे। जुआ खेलना सीखा और निहाल जैसा अनोखा दोस्त मिला। इसी बीच दोस्त के प्रभाव से एक समाज वादी शिविर में भीमताल आए और पहाड़ों का एक प्रभाव अपने मन पर ले गए जो आजन्म पहाड़-प्रेम में बदल गया। जीवन के अन्त में देहरादून आ बसने के पीछे शायद वह पुराना पहाड़ी स्पर्श भी रहा हो। देहरादून के चार साल उनके जीवन के अन्तिम साल थे। साल के जंगल के पास देहरादून के इस घर में वे जम गए थे और वाक़ई बहुत बार लल्दा (यह नाम उनको अजय रावत ने दिया था) ने अपनी ख़ुशी का इज़हार किया था।
1953 में हाईस्कूल यहीं आनन्द नगर से किया था। इस बीच दीदियों के घर जा ना भी होता पर अन्ततः अपने गोरखपुर आ गए। रामदत्तपुर के मकान में। यह घर शायद दादाजी के ज़माने में बना होगा। आज़ादी के बाद भी रामलीला, रिश्ते दारियों में तथा तराई फ़ार्म वाले जीजाजी के यहाँ जाना आदि चलता रहा। तभी उन्होंने तराई की तमाम ज़मीनों पर क़ब्ज़े होते, बसावटें बनते, विभाजन का दंश भुगतते लोगों को बसते और थारू जनजाति को उजड़ते देखा।
फिर गोरखपुर
इंटर और बी.ए. की पढ़ाई गोरखपुर में हुई। पूर्वांचल के सामान्य परिवार का यह बेटा छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो कभी बाद में शिक्ष क संघ का भी। कर्मचारी भी उन्हें अपना नेता मानते रहे। असल में उनकी मूल कामना थी कि सभी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी संगठित रहें ताकि जनता लड़ाकू बन सके, जिसका कि वे सभी हिस्सा हैं। 1957 में सेंट एंड्रूज से बी.ए. कर उन्होंने लखनऊ वि.वि. से एम.ए. (1959) और गोरखपुर विश्वविद्यालय से हरिशंकर श्री वास्तव के निर्देशन में डॉक्टरेट (1964) की। हरिशंकर उनके न्यारे गुरु रहे जो कुछ नाइत्तफ़ाकियाँ रखते हुए भी उनसे बहुत प्यार करते थे। लल्दा की आत्मकथा में इसका द्रवित करने वाला प्रसंग है। उन्होंने बलिया के सतीशचन्द्र पी. जी. कॉलेज में कुछ वर्षों तक पढ़ाया भी।
इसी बीच उन्हें फ़्रांसीसी सरकार का वजीफा मिला और वे सारबॉन विश्वविद्यालय एक बार फिर पढ़ने चले गए। उन्हें वहाँ रेमो ऑरों जैसे शिक्षक मिले, जिनके निर्देशन में उन्होंने ‘इतिहास-लेखन की समस्याएँ’ विषय पर शोध किया (1968)। वे सदा रेमो ऑरों का आभार जताते थे कि उन्होंने उन्हें इतिहास-दृष्टि के साथ जीवन-दृष्टि भी दी। उन्हीं के सम्पर्क और शिक्षण ने उन्हें इतिहास के विद्यार्थी और शिक्षक की महत्तम जिम्मेदारियों का भान कराया।
रेमो ऑरों (14 मार्च , 1905-17 अक्टूबर, 1983) बीसवीं सदी के महत्त्वपूर्ण फ़्रेंच बुद्धिजीवी थे। वे सार्त्र के सबसे बड़े मित्र और प्रति द्वंद्वी थे। प्रथम विश्वयु़द्ध, रूस की क्रान्ति , द्वितीय विश्वयुद्ध, 1968 का छात्र-विद्रोह और द गॉल के शासन आदि का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। उनकी किताब द ओपियम ऑफ़ द इंटेलेक्चुअल्स (1955) बहुत चर्चित रही, जिसमें उन्होंने कहा था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फ्रांस में मार्क्स वाद बुद्धिजीवि यों के लिए अफीम की तरह हो गया था। ये बुद्धिजीवी पूँजीवाद और जनतंत्र की तो तीखी आलोचना करते थे पर मार्क्सवादी व्यवस्थाओं में हो रहे दमन, ज़्यादतियों और असहिष्णुता को बख़्श देते थे।
ऑरों से उन्होंने अपनी भाषा में लिखने, बोलने और पढ़ने का मर्म समझा। यह किसी और भाषा का निषेध नहीं था बल्कि इसका अर्थ था कि जिस भाषा में सोचते हो, उसमें लिखो और बोलो। और पेरिस के अकादमिक जीवन को छोड़कर वे अपने मुल्क लौटे। इस तरह वे पढ़ाने को फिर गोरखपुर आए। वे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी और फ़्रेंच लिखते और बोलते थे पर पेरिस से इरादा बाँधकर लाए कि हिन्दी में बोलेंगे और लिखेंगे। यह उन्होंने आजन्म किया और डंके की चोट पर किया। उन्होंने अपनी डाक्टरेट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन नाइन्टींथ सेंचुरी इंडिया अंग्रेज़ी में लिखी तो सारबोन की थीसिस फ़्रेंच में लेकिन अपनी शेष सभी किताबें हिन्दी में लिखीं। अंग्रेज़ी तथा फ़्रेंच से उन्होंने बहुत सारा साहित्य हिन्दी में अनुवाद किया।

शिक्षक, शोध निर्देशक
एक शिक्षक, शोध निर्देशक तथा पाठ्यक्रम-निर्माता के रूप में उन्हें गोरखपुर विश्वविद्यालय (1969-1984), मणिपुर विश्वविद्यालय (1984-90), इलाहाबाद विश्वविद्यालय (1991-98) के साथ अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी याद किया जाता रहेगा, जहाँ उन्होंने इतिहास दर्शन तथा स्थानीय, क्षेत्रीय इतिहास जैसे प्रश्नपत्रों को पाठ्यक्रम में जोड़ने में योगदान दिया। उनके ज़्यादातर व्याख्यान ‘जन इतिहास’, ‘इतिहास में आमजन’ या मौखिक इतिहास की थीम पर होते। भारतीय इतिहास कांग्रेस में वे सदा सक्रिय रहे। इतिहास कांग्रेस के अलीगढ़ अधिवेशन (1994) में उन्होंने फ़्रांसीसी क्रान्ति पर फ़्रांसीसी इतिहास-लेखन की झलक दिखाने के बहाने ‘जन के लिए इतिहास’ का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था। उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस के संस्थापकों में वे एक थे। मुझे टांडा, उत्तर प्रदेश के छोटे से क़स्बे में उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस का संस्थापना अधिवेशन याद है, जिसके स्थानीय सचिव एस.एन.आर. रिजवी थे। उत्तराखंड इतिहास तथा संस्कृति परिषद की स्थापना में वे प्रेरक थे और इसके अध्यक्ष भी रहे। जब तक वे मणिपुर रहे, पूर्वोत्तर इतिहास कांग्रेस में भी सक्रिय रहे।
पत्रिकाएँ और सांस्कृतिक पहलें
उन्होंने सबसे पहले भंगिमा (1972) पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। मुझे भंगिमा में हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना की छवि दिखती थी। गोरखपुर तब सृजनशीलता का केन्द्र बन रहा था। अगले चार दशकों में गोरखपुर की प्रतिभाएँ पूरे देश में फैल गईं। पत्रिकाएँ, नाटक, चित्र प्रदर्शनियाँ, संगोष्ठियाँ और तरह-तरह के संवाद। इस सबमें विश्वविद्यालय की केन्द्रीयता स्वाभाविक थी। वहाँ के शिक्षकों का योगदान इस बौद्धिक-सांस्कृतिक गतिशीलता में था। बी.एन. झा, कामेश्वर सहाय भार्गव, विशुद्धानन्द पाठक, हरिशंकर श्रीवास्तव, गिरीश रस्तोगी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डी.पी. धूलिया, केदारनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव आदि लोग इसमें शामिल हुआ करते।
प्रकाशन-सम्पादन की यात्रा फिर लोक चेतना तथा इतिहास-बोध की ओर आई। इतिहास-बोध अभी हाल हाल तक प्रकाशित होती रही। इतिहास अध्ययन तथा इतिहास निर्माण के लिए कितनी ही पुस्तिकाएँ वे निकालते रहे। 1978 में उन्होंने प्रेमचन्द के गाँव में राष्ट्रीय जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का गठन किया। 1984 में देश में सांस्कृतिक आन्दोलन की दिशा को लेकर तमाम संस्कृति कर्मियों का सम्मेलन कराया। प्रेमचन्द , राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या अदम गोंडवी के स्मृति समारोह उनके मूल स्थानों में जा कर या अन्यत्र करने की हिम्मत उनमें और उनके साथियों में थी। सन्धान के सम्पादन में भी वे सुभाष गाता डे तथा मित्रों के साथ जुड़े थे। वे दशकों तक साहित्य और इतिहास के बीच के पुल, नाव और परिचयकर्ता बने रहे।
‘संचेतना’ जैसा नाट्य तथा सांस्कृतिक दल उनके निर्देशन में बना और अनेक नाटक भी उन्होंने लिखे। जब जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रेस पर पाबन्दी लगाने की कोशिश की। इसका बिहार और देश में विरोध हुआ। ‘संचेतना’ ने तय किया कि इसका सांस्कृतिक तरीक़े से विरोध कि या जाए। लाल बहादुर ने एक नुक्कड़ नाटक लिखा ‘ताला ज़ुबान पर’ और संचेतना की टीम जगह-जगह नाटक करती हुई पटना तक गई। नाटक को सैकड़ों लोगों ने देखा और इसकी मुद्रित प्रति ख़रीदी भी। बिहार के पढ़ाकूपन को उन्होंने इस यात्रा में महसूस कि या, जब एक दसेक साल के बच्चे ने भी नाटक की प्रति ख़रीदी।

किताबों का सिलसिला
फिर उनके एक मित्र ने मैकमिलन से हिन्दी प्रकाशन शुरू होने पर उनसे सरल हिन्दी में यूरोप का इतिहास (दो खंड) जैसी मौलिक किताब लिखवा ली, जिसे विद्वान और विद्वान बनना चाहने वालों के अलावा सामान्य पाठक भी पढ़कर लाभान्वित हो सकते थे। वर्ना हिन्दी में यूरोप के इतिहास पर दोयम दर्जे की किताबें ही थीं। लेखन का यह सिलसिला चलता रहा। दो भागों में आधुनिक विश्व इतिहास, इतिहास : क्यों-क्या-कैसे?, अधूरी क्रान्तियों का इतिहास बोध (2009), क्रान्तियाँ तो होंगी ही, इतिहास के बारे में, कांग्रेस के सौ साल, अपने को गम्भीरता से लें, भारत की जनकथा (2012), मानव मुक्ति कथा, गांधीगिरी बनाम दादागिरी और गुलामगिरी, धरती हमारी माँ: संवेदना और समझ का वैश्विक परिप्रेक्ष्य आदि अनेक किताबें लिखीं।
देहान्त से पहले उनकी एक किताब आज़ादी का मतलब क्या तैयार थी। अगली किताब वे फ़ासीवाद पर लिख ना चाहते थे। अगले जाड़ों में केरल जा ने पर वे महात्मा गांधी पर भी एक किताब लिखना चाहते थे। गांधी को वे नई और खुली नज़र से देखने को उत्सुक थे। आख़िर उस व्यक्ति की अदम्य ऊर्जा और मौलिकता का स्रोत कहाँ था, यह वे जानना चाहते थे। पिछली बार गांधी पर राम गुहा की किताबों की चर्चा उन्होंने की थी, जब मैंने उनको बताया था कि गांधी के 150 साल होते समय उनकी उत्तराखंड की यात्राओं के 90 साल हो रहे हैं। उनसे कहा कि गांधी के 1929 के बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर तथा हरिद्वार-देहरादून-मसूरी मार्ग में एक चेतना यात्रा का आयोजन होना चाहिए। वे इस हेतु बहुत उत्साही थे। पर 2019 में यह सम्भव नहीं हुआ और फिर कोविड का दौर शुरू हो गया।
लल्दा की तीन औपन्यासिक और दो आत्मकथात्मक किताबें ख़ूब चर्चा में रहीं और बनी रहेंगी। उत्तर पूर्व, मई अड़सठ, पेरिस और जिंदगी ने एक दिन कहा यह उनके तीन उपन्यास हैं। पहली रचना उनके मणिपुर के अनुभवों पर आधारित थी। हिन्दी साहित्य में पूर्वोत्तर उसी तरह अनुपस्थित है, जिस तरह इतिहास में। वहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधता औसत भारतीय बहुत कम जानता है। पूर्वोत्तर की अस्मिता को न जानने के कारण वहाँ की स्वायत्तता की समझ भी शेष भारत को कम है। इसलिए उनकी स्वायत्तता की लड़ाई को उस पूरे क्षेत्र का विद्रोह समझ लिया जाता है। शेष भारत वहाँ फ़ौज तथा पैरा मिलिटरी के साथ चाय बाग़ानों के मालिकों-मज़दूरों या ओ.एन.जी.सी. की यूनिटों के रूप में मौजूद है। यह उपन्यास उस दृष्टि-ठहराव को तोड़ने की कोशिश है। हालाँकि पूर्वोत्तर की विविधता का पूरा भान उन्हें नहीं हो सका, ऐसा वे बार-बार जताते थे। अब हिन्दी में मुश्किल से कुछ यात्रा संस्मरण पूर्वोत्तर पर आने लगे हैं। भारत की आने वाली पीढ़ियाँ पूर्वोत्तर की विविधता को समझेंगी और नाज़ करेंगी।
दूसरा उपन्यास था पेरिस के छात्र विद्रोह पर, जिसके ताप को उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था , जिसकी अनुगूँज को वे पेरिस प्रवास में लगातार सुनते और गुनते रहे। पेरिस की 1789, 1871 और 1968 की घटनाएँ इस शहर और देश की जीवंतता और बेचैनी का संकेत देती थीं, जिन पर उन्होंने बड़ी अनुभव-सम्पन्नता से लिखा। इतिहास के विद्यार्थी की हैसियत से उन्होंने फ़्रांसीसी क्रान्ति और पेरिस कम्यून पर पर्याप्त प्रकाश डाला। यह इतिहास को महसूस करके लिखने जैसा था। 1991 में मुझे एक सम्मेलन में 15 दिन पेरिस में रहने का मौक़ा मिला। संयोग से हमें ‘होटल बैस्टी ल’ में रहना था, जो ऐतिहासिक बैस्टील के किले के बिलकुल पास था। मैंने क्योंकि उनकी किताबें पढ़ी थीं और उनसे बहुत कुछ सुना था तो मुझे उस इतिहास के पात्र और घटनाएँ जैसे साक्षात् दिखती रही थीं। एक वालंटियर ने जब हमें बताया कि यहाँ पर नेपोलियन ने भाषण दिया था तो मुझे लल्दा की याद आई।
उनका तीसरा उपन्यास जिंदगी ने एक दिन कहा भोपाल गैस कांड पर था। 1984 की 2-3 दिसम्बर को यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में दुनिया की सबसे मारक औद्योगिक दुर्घटनाओं में एक हुई थी। सरकार या कम्प नी के अनुसार तो लगभग 4 हज़ार पर ग़ैरसरकारी अनुमानों के अनुसार 15 हज़ार से अधिक लोग इसमें मारे गए। साढ़े पाँच लाख की जनसंख्या किसी न किसी रूप में प्रभावित या अपाहिज हुई। आज तक भी न पीड़ितों का पुनर्वास हुआ और न उनको पर्याप्त मुआवज़ा मिल सका (इस कांड की चेतावनी देने वाले पत्रकार राज कुमार केसवानी का पिछले सप्ताह कोरोना से भोपाल में देहान्त हो गया है)। पहले इसका नाटक रूप प्रस्तुत हुआ था। पर अन्ततः इसका औपन्यासिक रूप सामने आया। यह उनकी उस गहरी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति थी। हुआ यह था कि अभिनेत्री सुहासिनी मुले कि सी फिल्म शूटिंग के लिए भोपाल आई थीं, जब यह हादसा हुआ। सुहासिनी की संवेदना और समझने उनको फिल्म का काम रोक, राहत के काम से जोड़ दिया। इस घटना को वे ही पकड़ सकते थे। यह दुर्लभ गुण ही उन्हें लाल बहादुर बनाता था ।
उनकी आत्म कथा के दो खंड कम से कम सात -आठ दशकों के बहुत से समय-आयामों को हमारे सामने रखते हैं। पहले खंड को उन्होंने शीर्षक दिया था जीवन प्रवाह में बहते हुए (2015) और दूसरे को बुतपरस्ती मेरा ईमान नहीं (2019)। बहुत खुली है उनकी आत्म कथा । इन किताबों का उनकी मुस्कुराहट से ताल्लुक़ है। यानी उनके खुलेपन से। भारतीय क़स्बाई मध्य वर्ग से निकला व्यक्ति किस तरह बनता है, इस प्रक्रिया को शायद ही उन्होंने कहीं छिपाया हो। यह पारदर्शिता उनकी ऊँचाई को बनाती रही। वर्ना मध्य वर्ग के लिए किसी ऊँचाई को बुद्धिजीवी होने के बाद भी गढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जब वे धारा के साथ बह रहे थे तब भी वे तैर रहे थे और कभी-कभार धारा के विरुद्ध भी।
इसके बाद उनका योगदान सचेष्ट और सक्रिय अनुवादक के रूप में रहा। वे तमाम देशों और भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य को विश्व-धरोहर मानते थे। इसलिए उन्होंने अनेक साहित्यिक और ऐतिहासिक किताबों का हिन्दी अनुवाद किया। उनमें एरिक हॉब्स बाम के सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ क्रान्ति का युग (एज ऑफ़ रिवोल्यूशन) 2009; विक्टर ह्यूगो के उपन्यास विपदा के मारे (ले मिजेरबल); जैक लंडन के उपन्यास आईरन ह्वील; हावर्ड फास्ट के चार उपन्यास तीन क्रान्तियों का प्रवक्ता (सि टीजन टॉम पेन), वासन्ती सुबह (अप्रैल मार्निंग), अपराजित (अनवैंक्वि स्ड) तथा अमेरिकन; आर्थर मारविक की नेचर ऑफ़ हिस् ट्री , क्रिस हर्मन की पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ़ द वर्ल्ड तथा चेंजिंग वर्ल्ड विदआउट पावर और हॉवर्ड जिन के कुछ अंश तथा बॉब डिलन के कुछ गीत प्रमुख हैं। फ़्रेंच से उन्होंने फुटकर तो कई लेख, कविताएँ अनूदित कीं पर एंतोनी डी सेंत की नन्हा राजकुमार बहुत प्रसिद्ध हुई।
कितना कुछ वे अभी भी कर रहे थे। दरअसल जब वे कहते थे कि आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी वे कुछ न कुछ कर रहे होते थे। जब वे जाड़ों में दक्षि ण और गर्मि यों में पहाड़ों में कहीं एक-दो माह रहते तो कोई न कोई पांडुलिपि बनकर उनके साथ वाप स लौटती थी। साथ ही वे उस ठौर पर दोस्त बनाकर और बढ़ाकर आते थे।

खनिज और मिश्र धातुएँ
वे भी तरह-तरह के खनिजों से बने व्यक्ति थे। इतिहास तथा साहित्य को उनकी मुख्य खनिज चट्टा नें माना जा सकता है। अपने होने को सिद्ध करने की कुछ मिश्र धातुएँ उन्होंने ख़ुद बनाई थीं जैसे प्रकृति प्रेम, पर्यावरण बेचैनी, उपभोग की अति की निरर्थकता, अध्यात्म को नए सिरे से समझना और गांधी तथा आंबेडकर को भी। सहृदयता और प्यार बाँटते चलो का फ़लसफ़ा उनकी एक अलग राह बना देता था। यह सोच-समझदारी उन्हें ‘मठी मार्क्स वादियों’ से अलग करती है। इसलिए उनकी मुख्य रुचि तमाम मुद्दों के लिए मुहिम, जनजागरण और जनान्दोलनों की तैयारी की रही। जन इतिहास की वकालत इसीलिए वे ताजिन्दगी करते रहे। वे अतीतग्रस्तता की नहीं सदा इतिहासबोध की बात करते रहे। वे यह भी कहते रहे कि हर क्रान्ति असफल हुई लेकिन फिर भी उसने मनुष्यता को आगे बढ़ाया। इसे ही वे आदमी से इनसान बनना या जैविक से सांस्कृतिक इनसान बनना कहते थे और ऐसा इनसान बनाना उनका लक्ष्य और गन्तव्य रहा। स्वाभाविक ही इसमें कोई निश्चित पार्टी लाइन लेनी सम्भव नहीं थी। इसी तरह के संकट से सक्रिय समाज वादी और हरफनमौला कृष्ण नाथ भी गुज़रे थे।
सत्य को समझना और उसका साथ देना, अन्याय का विरोध करना, मानवीयता का पक्ष लेना वे ज़रूरी मानते थे। इस त्रिभुज के बीचोंबीच एक दिल का निशान होता था। यानी वे इसे मुहब्बत से जोड़ते थे। आदान-प्रदान और संवाद से जोड़ते थे। लगातार कहते थे कि हर जिन्दगी में प्यार के लिए, उसे पाने और देने के लिए पर्याप्त समय और जगह होनी चाहिए। इसीलिए वे अन्त में अपने विद्यार्थियों में अपना गुरु ढूँढ़ते थे। उनके अनेक विद्यार्थी भी उनके व्यक्तित्व के अनेक कोने-अँतरों से परिचित नहीं थे। वे उतना ही जानते थे, जितना दिखता था। मुझे उनका अपने आप को छिपाना अनेक बार पकड़ में आया था। आत्म कथा तो उनकी अब आई है।
देश या विदेश में हमें सैकड़ों ऐसे छात्र, शिक्षक, अधिकारी, पत्रकार, रचनाकार और नागरिक मिल जाएँगे जिनको लाल बहादुर ने अपनी मुहब्बत से विचार और कार्यक्रमों से जोड़ा। यह तमाम लोग अनेक सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक पृष्ठभूमियों से उगे और आए हो सकते हैं। मैं दर्जनों ऐसे नाम गिना सकता हूँ जो इस संसर्ग से विकसित हुए। राजेश मल्ल, महेंद्र प्रताप, सैयद रज़ा रिजवी, रवि प्रकाश सिन्हा, कंचन सिन्हा, शशि प्रकाश, कात्यायनी, विकास नारायण राय, बद्री नाथ (गोरखपुर); बद्री नारायण, ललित जोशी, राकेश कुमार गुप्ता, रमाशंकर सिंह, मृत्युंजय, अंकित पाठक (इलाहाबाद); पंकज श्रीवास्तव (दिल्ली), हितेन्द्र पटेल (कोलकाता); गिरिजा पांडे (नैनीताल); गौरव नौटियाल, अरविंद शेखर, गीता गैरोला (देहरादून) आदि कितने ही नाम लिये जा सकते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में ज्ञानोदय और प्रबोधन के काम आगे बढ़ाए हैं। ये सहयोगी, वि द्यार्थी और सहकर्मी उनके अन्त रंग दोस्त बन गए। आज़ादी बचाओ आन्दो लन के बनवारीलाल शर्मा से उनकी दोस्ती भी अपनी तरह की अनोखी थी।
वे अपने को इतिहास-चेतना का प्रचारक मानते थे। कभी जब हम कहते थे कि ‘प्रचारकों’ ने तो इस देश में तार्किकता को ख़ारिज कर साम्प्रदायिकता को पाल-पोस लिया है वे कहते कि खुलकर अपनी बात रखना किसी भी प्रचारक के लिए ज़रूरी है। देर-सबेर सत्य और तार्किकता की जीत होगी। यह भी कहते थे कि दुष्प्रचार और झूठ चाहकर भी बहुत दिन नहीं टिकते हैं। इसके लिए वे दोस्ती ज़रूरी मानते थे। वे अलग ही किस्म के वामपंथी थे। आज़ाद, अत्यन्त उदार और लचीले। वे किसी और अच्छी विचारधारा के मिलने पर प्रचलित वामपंथ को भी छोड़ने को तैयार थे। यह उनके सोच की पराकाष्ठा थी, जो साँचे में ढली अधिकांश साम्यवादी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वालों को पसन्द न थी।
मैंने किताबें बेचते हुए या तो कुछ बार इरफ़ान हबीब और हर बार लाल बहादुर वर्मा को देखा। वे तो तरह-तरह की चीज़ें बेचते थे। छोटा फोल्डर, पोस्टर, पुस्तिका, पुस्तक या पत्रिका। जैसे अनुपम मिश्र को पर्यावरण का ‘सबसे बड़ा बाबू’ या ‘सबसे बड़ा मास्टर’ कहा जाता था, वैसे ही जन साहित्य और जन इतिहास के वे हिन्दी पट्टी में ‘सबसे बड़े बाबू’ या ‘सबसे बड़े मास्टर’ थे। पर वे नाटक में हिस्से दारी कर सकते थे और कोरस में भी। रसोई में जा कर खाना बनाने या बर्तन मलने में उनको दिक़्क़त न थी। इसी बीच फ़ुर्सत मिलते ही वे एक सिगरेट भी पी सकते थे। इसी तरह अनुपम भी कितने ही गुणों की खान थे।
7 दिसम्बर, 2013 को दिल्ली के गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में राहुल सांकृत्यायन व्याख्यान के मौक़े पर लगभग पाँच घंटे अनुपम दा, लल्दा और मैं साथ रहे। तीन घंटे तो हम तीनों ही बतियाते रहे। यह गपशप मैं कभी नहीं भूलूँगा। दोनों एक-दूसरे के विचार संसार तथा अर्जित समझदारी में घुसना चाहते थे और दोनों को लगता था कितनी सारी चीज़ें उनकी उभयनिष्ठ हैं। एक जन गांधी के रास्ते पर्यावरण के झमेले को समझ रहा है दूसरा मार्क्स के, पर दोनों मान रहे थे कि समाज भी अपने स्तर पर टिके रहने के रास्ते खोजता है, उनका आविष्कार करता है। मार्क्स और गांधी से पहले भी ये समाज अपनी हिफ़ाज़त के रास्ते खोज रहे थे और पा भी रहे थे। हिमालय को भी अनेक तरह से देखने की अपेक्षा दोनों मुझसे कर रहे थे। हिमालय को क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों तरह से देखने की पद्धति दोनों को सुहाई।
कितने अवयवों से बनता है कोई पता नहीं और कौन-कौन से अवयव थे उनमें! शायद कुछ से हमारा या अन्य मित्रों का वास्ता ही नहीं पड़ा था। शायद 1977 की बात थी। आपात काल अभी नहीं हटा था। गुरुनानक देव विश्वविद्यालय में इतिहास पाठ्यक्रम की कोई कार्यशाला थी। मैं अपनी शिक्षक शाकंबरी जयाल के साथ और वे अपने शिक्षक हरिशंकर श्री वास्तव के साथ वहाँ पहुँचे थे। लगभग सप्ताह-भर हम साथ रहे। हम दोनों हिन्दी में एक जैसा बोल रहे थे। वे तथ्य-प्रधान और मैं भावना-प्रधान। हरिशंकर जी ने पूछा लाल बहादुर को कब से जानते हो? मैंने कहा कि अभी तो मिले हैं पहली बार। वे मुस्कुराए थे। मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनको भी यह पता नहीं था कि मैं अभी रंगरूटी कर रहा हूँ। मुझे अभी दो साल भी प्रवक्ता बने नहीं हुए हैं। पर हमारी कई बातें कद्दावर इतिहासकारों को नोटिस करने लायक़ लगीं। 1977 में वे एक दोस्त की तरह मेरे जीवन में आए, जल्दी ही वे मेरे शिक्षक बनते चले गए। 16 मई, 2021 को मैंने अपने दोस्त -शिक्षक को विदा किया।
लल्दा से आप भिखारी ठाकुर, बॉब डिलन, फ़ैज़, नाजिम हिकमत, गिर्दा या भूपेन हजारिका को एक साथ सुन और गुन सकते थे और इस संगीत के बाद भर्तृहरि, ब्रेष्ट या नेरुदा या बाबा नागार्जुन की कोई कविता। जब वे दो साल गोलूछीना (जिला अल्मोड़ा में द्वाराहाट के पास) आए तो हमने वीरेन डंगवाल के ‘आएँगे उजले दिन ज़रूर आएँगे’ गीत को उनके साथ गाया था। पर वे ‘जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियाँ बहती रहेंगी…’ को गाना कभी नहीं भूलते थे। अपनी प्रतिभा के इतने प्रकारों को वे बहुत सहजता और स्वाभाविकता से प्रकट होने देते थे। कहीं घूमने जाने में या घूमते हुए किसी जनगीत में शामिल होने में उन्हें कोई दिक़्क़त न थी।
गोरखपुर, लखनऊ, पेरिस, इम्फाल, इलाहाबाद, दिल्ली, करनाल, फरीदाबाद, देहरादून आदि जिन क़स्बों-शहरों में वे रहे, वहाँ उनकी दोस्ती अनेक स्तरों पर थी। उनसे असहमत हो जाने वाले भी उनसे बात करते थे और उनके बिलकुल प्रतिपक्षी भी उनकी निर्भीकता और धैर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। आपा खोना तो उन्होंने सीखा ही नहीं, ग़ुस्सा प्रकट करना भी बाद में वे भूल ही गए थे। वे विचार की लाइन तो ले सकते थे पर पार्टी लाइन उनके लिए सम्भव न थी। लकीर का फकीर बनना भी उनको स्वीकार्य नहीं था। मुक्त बुद्धिजीवी या संस्कृति कर्मी या जन इतिहासकार या इनका मिला-जुला रूप ही वे हो सकते थे और हुए। ऐसे लोगों की ज़रूरत भी इस देश और दुनिया को रहेगी। जैसा कि वे जीवन-भर करते रहे उसका सार मनुष्यता को पूँजी, रंगभेद, साम्प्रदायिकता, असमानता, अपमान, जाति-लिंग और क्षेत्रीय भेदभाव से बचाए रहने से जुड़ा था। प्रकृति की सुरक्षा, सही और सन्तुलित इस्तेमाल के वे अन्तिम सालों में बहुत बड़े समर्थक बन गए थे। अपनी अन्तिम एक किताब में धरती के लिए माँ शब्द उनके अन्तरतम से निकला लगता है।
उन्होंने तमाम महापुरुषों की जीवनगाथा सुनाने का क्रम भी शुरू किया। भगत सिंह और आंबेडकर पर तो प्रस्तुतियां हो भी गई थीं। देश के आन्दोलनों से वे कभी अलग नहीं हुए। शाहीन बाग जाने को वे बेचैन रहे पर किसान आन्दोलन में तो वे हो ही आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और उसके विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के समर्थन तथा वहाँ हो रही सत्ता-समर्थित गुंडागर्दी के विरोध में आयोजित देहरादून की जनसभा में शामिल हुए थे। ऑपरेशन के बाद उनको इधर-उधर जा ना मना था। पर वे वॉकर लेकर आए और सभा को सम्बोधित किया। देहरादून में तो उन्होंने एक नई सक्रियता पैदा कर दी थी। उनका इन तमाम वर्जित कोनों-अँतरों में नज़र डालना उनके कृतित्व को एक अतिरिक्त ऊँचाई देता है।
अब जब वह शरीर से नहीं रहे तो सबसे ज़्यादा ख़ालीपन तो स्वाभाविक रूप से रजनीगंधा भाभी, बेटी आशू, बेटे सत्यम और जमाई दिगम्बर को लगेगा। जैविक, भौतिक और पारिवारिक रिश्तों की गहराई और मिठास जिन लोगों में ज़्यादा होती है वहाँ उसी अनुपात में उदासी और सूनाप न प्रकट हो सकता है। रजनीगंधा भाभी कैंसर से भी लड़ रही हैं। पर इसे सिर्फ़ लाल बहादुर पद्धति से ही नियंत्रित किया जा सकता है। यानी चारों तरफ़ प्यार और दोस्ती । गोरखपुर में हिमालय के पाद प्रदेश की मिट्टी से विकसित यह लाल देहरादून में हिमालय और शिवालिक के बीचोंबीच फिर उसी मिट्टी में मिल गया वह बीज और उर्वरता हमारे बीच छोड़ गए हैं। नई ऊर्जा को अंकुरित होना ही चाहिए।

पहाड़ के संपादक व संस्थापक शेखर पाठक प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक हैं। वे कुमाऊँ विश्वविध्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। वे नेहरू मेमोरियल म्यूज़ीयम, नई दिल्ली व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के फ़ेलो भी रहे हैं। पहाड़ों के गहन जानकार, उन्होंने पहाड़ों को समझने से लिए कई यात्राएँ की एयर लगभग सभी असकोट आरकोट यात्राओं में भागीदारी की।