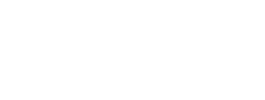काफी समय से मेरी तिब्बत जाने की योजना थी। गढ़वाल के सरहदी गावों के व्यापारी हर वर्ष तिब्बत जाते थे। वे जुलाई में वहाँ जा अक्टूबर तक व्यापार करते और बर्फ पड़ने से पहले वापस लौट आते। भारत से वे गुड़, चीनी, कपड़ा, तंबाखू, बर्तन, खाने-पीने और रोज़ाना इस्तेमाल का सामान ले जाकर बेचते और वहाँ से नमक, ऊन, सुहागा और कभी थोड़ा सा सोना खरीद लाते।
मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करने लगा था। देवदासजी हमारे प्रमुख थे। मैंने उनसे यात्रा हेतु अपनी सब जमा छुट्टी 1952 के जून महीने में देने का निवेदन किया। देवदासजी ने शुरू में कहा कि यदि तुम जा रहे हो तो अखबार के लिए कुछ लिखना। लेकिन उनके श्वसुर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की राय थी कि भारत-चीन के बीच तिब्बत के मामले पर तनाव के कारण हिन्दुस्तान टाइम्स को वहाँ संवाददाता भेजना उचित नहीं होगा।
चीन किसी को भी तब तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं देता था। यदि मैं भारतीय व्यापारियों के साथ गया तो चीन उस पर आपत्ति कर सकता था और यदि मुझे वहाँ पकड़ लिया गया तो वह कह सकता था कि मैं अवैध रूप से आया हूँ। लेकिन मैं तो किसी भी हाल में जाना चाहता था। मैंने कहा मुझे जाना ही है तो देवदासजी ने आखिरकार छुट्टी दे दी!
तिब्बत जाने के लिए मैं प्रसिद्ध तीर्थ श्री बदरीनाथ से तीन मील आगे भारत के आखिरी सरहदी गाँव माणा पहुँचा। वहाँ जून अंत में तिब्बत जाने वाले व्यापारियों की तैयारियाँ चल रही थीं। पहला काफिला सफेद बालों वाली बड़ी बकरियों की पीठ पर सामान लाद कर चलने को तैयार था। इस यात्रा में सामान लदे बड़े जानवर, खच्चर, घोड़े, याक, इत्यादि नहीं ले जाए जाते थे। आक्सीजन की कमी के कारण कई बोझा लदे जानवर चढ़ाई चढ़ने में अक्सर मर जाते! बकरी हल्की थी और आसानी से चढ़ाई पर सामान ले सकती थी। हर बकरी 15 किलो भार ले जाने में सक्षम थी।
हमेशा की तरह व्यापार खोलने एक तिब्बती अधिकारी, जिसे सरजी कहते, भारतीय सरहदी गावों में आता। उसका पहला काम होता कि वह पता लगाए कि सरहदी गांवों में जानवरों को खुर की बीमारी तो नहीं है जो तिब्बत पहुँचने पर वहाँ के जानवरों को बडी संख्या में मार सकती है।
सरजी गाँववालों को बुलाकर उनसे लिखवा लेता कि उस क्षेत्र में जानवरों को खुर की या अन्य कोई बीमारी नहीं है़। उसके बाद ही उस साल व्यापार करने पर समझौता किया जाता़। सरजी गाँववालों से एक पत्थर मंगवाता। सबसे के सामने इसके दो भाग किए जाते और उन्हें कपडे में लपेट सील-बंद किया जाता। उनमें एक गाँववालों को दिया जाता और दूसरा सरजी अपने पास रख लेता। यदि यह पता चलता कि गाँववालों ने अपने क्षेत्र में जानवरों की बीमारी को छिपाया है जिसके कारण बीमारी तिब्बत में पहुँच कर फैली तब वह गाँववालों को बुला उनसे वह पत्थर का सील किया टुकड़ा मंगवाता और अपने पास वाले टुकड़े से उनका मिलान करता। इस तरह बीमारी के बारे में जिस ओर से झूठ बोला गया हो उसको दंड के रूप में उस पत्थर के भार के बराबर सोना दूसरे को देना पड़ता। इस औपचारिक समझौते के बाद सरजी व्यापार खोल देता था।
मैं सामान लदी 2500 बकरियों और उनके दस हाँकने वालों के काफिले के साथ माणा गाँव से अपनी लंबी तिब्बत यात्रा पर जुलाई 1952 में निकला था। बकरियों पर सामान लादना, उतारना आसान होता था। जब बर्फ का कोई ढलान आता तो कुछ हांकने वाले ढलान पर बैठ-फिसल नीचे उतर जाते, फिर ऊनी थैलों जिनमें माल भरा होता उन्हें बर्फ पर नीचे फिसलाया जाता। इसी तरह बकरियों को बर्फ पर लिटा, धीरे से नीचे की ओर फिसलाया जाता जहाँ उनको पहले से वहाँ पहुँचे लोग पकड़ लेते। एक बार फिर उनपर सामान के फांचे (थैले) लाद काफिला आगे चल देता।
तेज़ी से बहती पतली सरस्वती नदी के किनारे खड़ी कठिन चढाई चढ़ हम दो दिन में 18,400 फीट ऊंचे माणा धूरा (पास) पहुँच गए। जून की गर्मी ने वहाँ कुछ बर्फ गला दी थी तथा जुलाई आरंभ की वर्षा ने उसे नीचे बहा दिया था। तब भी ऊँचाइयों पर वह गहरी थी जिसमें हमारे पाँव धँस जाते। आक्सीजन की कमी के कारण श्वास लेना कठिन था। धूरा दोपहर से पहले पार करना होता क्योंकि दोपहर बाद बर्फ की इतनी आंधी चलती कि कुछ दिखाई नहीं देता था।
धूरे पार तिब्बत के पहाड इतने तीखे और ऊँचे नहीं थे जितने भारत के। वे रेतीले, सख्त हरी घास भरे होते और उन पर झुण्ड के झुंड ज़ेब्रा जैसी धारियों वाले तिब्बती जंगली गधे, जिन्हें क्यांग कहा जाता, चर रहे होते। उनके पास जाने पर वह दौड़ कर रेत का बादल उडाते हुए भाग जाते। अन्य जंगली जानवर, जैसे खरगोश, बहुत गर्म और मुलायम ऊन की जंगली तिब्बती भेड़ तथा कभी भेड़िया भी दिखाई देते।
इस यात्रा में कई दिनों तक तिब्बत में एक घर भी नहीं दिखाई दिया। रेतीले ढलान खेती योग्य नहीं थे। रात को किसी ढलान में तंबू लगा कर हम लोग सो जाते। बकरियों को चराने के बाद डंडों और रस्सियों की एक बाड़ बना कर उसमें उन्हें रख दिया जाता। तिब्बत में एक छोटा बाघ, जिसे वहाँ के लोग चांकू कहते वह रात में चुपके से बाड़े में घुस आता और कई बकरियों को मार देता। वह उनका मांस नहीं खाता, केवल खून पीता! हमारे साथ बकरियों की रक्षा के लिए खूंखार कुत्ते होते थे। तब भी सुबह के अंधेरे में जब हम उठते तो दो-चार बकरियाँ चांकू द्वारा मारी गईं पाते!
ढलानों पर उतर तीसरे दिन हम सतलज नदी के किनारे स्थित बडे थोलिंग मठ पहुँचे। वहाँ का बडा लामा चीनियों के डर से राजधानी ल्हासा भाग गया था, लेकिन तब भी बहुत से लामा वहाँ थे। वह एक बहुत ही भब्य और बडा मठ था, प्राचीन, सुंदरतम मठों में एक। उसकी सभी दीवारों पर बुद्ध और तांत्रिक देवी देवताओं, जैसे काली तथा महाकाल, के बडे रंगीन चित्र बने थे। नदी पर लकड़ी का संकरा पुल था और उसके किनारे छोटे खेत जिनमें जौ, मटर और मूली उग रहे थे।
यह तिब्बत की पुरातन, पहली राजधानी, गूगे के निकट था। रास्ते में तीन और रात तंबुओं में बिता चौथे दिन हम पश्चिमी तिब्बत की राजधानी गरतोक पहुँचे। जिन माणा व्यापारियों के साथ मैं आया था यह उनकी मंडी थी। यहीं वे अपने तंबू गाड उनमें दुकानें सजाकर अपना सामान बेचते या अद्ली-बदल करते थे। वे भेड़ का ऊन खरीदते और उसे भारत लाते।
भारत की सरहद के विभिन्न भागों से आए व्यापारियों को तिब्बत में अलग-अलग, निश्चित स्थानों में मंडियाँ लगाने की आज्ञा थी, जहाँ वह तीन-चार महीने रह व्यापार कर सकते थे। आस-पास के गावों में उनके तिब्बती ‘मित्र’ होते, जिनके पास वह अपनी बकरियाँ, याक तथा जो सामान बिक नहीं पाया उसे लौटते समय छोड़ आते।
भारत के व्यापारी वहाँ से नमक लाते थे। भारत के उत्तरी सरहदी क्षेत्रों से पश्चिमी भारत का नमक बनाने वाला भाग बहुत दूर पड़ता था और नमक को गाँवों तक लाने के लिए न रेल थी न सड़क। इसलिए भारत तथा नेपाल के सरहदी गाँव तिब्बत से लाए नमक पर आश्रित थे। इस नमक का उस सरहदी क्षेत्र में बड़ा व्यापार था। तिब्बत के नमक के मैदानों के उत्तर-पश्चिम में एक छोटी-सी सोने की खान थी, जहाँ खोदने पर सोने के कण मिल जाया करते थे। तिब्बती मज़दूर वहाँ गड्डे खोद सोना खोजने में लगे रहते। भारतीय व्यापारी भी कभी कभार वहाँ से कुछ सोना खरीद ले आते। एक अन्य वस्तु जो तिब्बत में काफी मात्रा में मिलती वह था सुहागा। भारत में सुहागा सोना तथा अन्य धातुओं के शोधन के काम आता इसलिए यहाँ उसकी अच्छी माँग थी।
तिब्बत में गाँव-घर ढलानों पर बने थे। ठंड से बचने के लिए वो आधे पहाडों के अन्दर, गुफाओं की तरह, और आधे बाहर होते। दीवारें मिट्टी की होतीं। सभी पुरुष, स्त्रियाँ, बच्चे भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनते जो कमर पर बंधा रहता। खाल का बाल वाला भाग अंदर की ओर होता। ऊनी हाथ के बुने कपड़े के पायजामे और रस्सियों के तले वाले ऊनी घुट्ने तक के बूट सब पहनते थे। साबुन न होने के कारण पहनावा धोया, बदला नहीं जाता जब तक वह फट कर तार-तार हो फेंकने को न हो जाए। लोग पसीने की बदबू से सने होते। कमरबंद के ऊपर खाल का कोट काफी ढीला रहता और उसके अंदर लोग लकडी का एक बडा कटोरा और अन्य वस्तुएँ रखते।
रेतीली ढलान पर खेती नहीं होती थी। नदियों के किनारे कुछ छोटे खेत थे जिनमें जौ, मटर, मूली और कुछ सब्जियाँ उग रही होतीं। लोग जौ को भून सत्तू बना, खाते। भर पेट शायद कम को ही भोजन मिलता। लोग कम खा जीवित रहने के आदी हो चले थे।
यूँ तो तिब्बत बौद्ध धर्मानुयाई था तब भी कुछ थे जो भेड-याक मार उनका मांस खा या बेच लेते थे। उनकी बस्तियाँ अलग थीं। यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम थी। इसका एक बड़ा कारण था प्रत्येक परिवार को एक बच्चा लामा या भिक्षुणी बनने मठों को देना होता। वे सारी उम्र कुवांरे रहते और दूसरा बडा कारण था बहुपति प्रथा का चलन।
सारे तिब्बत में केवल चार किलोमीटर मोटर सडक थी, जो दलाई लामा के शीतकालीन महल पोटाला से ग्रीष्मकालीन महल, नोरबूलिंका तक जाती थी। मोटर गाडी भी 1950 तक देश में एक ही थी, जिसपर बैठ दलाई लामा अपने इन दो महलों को आते-जाते। अच्छी खेती की भूमि या तो मठों के पास होती या बडे अधिकारियों-सामंतों के पास। बाकी लोग दास थे जो, कुछ अन्न पाने के लिए, सारे समय सपरिवार सामंतो और मठों के लिए बिना वेतन काम करते।
बडे परिवार के बच्चे लामा बनते, जिन्हें पूजा-पाठ के अलावा कुछ काम नहीं करना पडता। निम्न परिवारों के बच्चे, लामा बन मठों में खाना पकाना, झाडू-सफाई तथा खेतों में काम, बिना वेतन के करते थे। दंड पाए लोगों के दोनों पैर लकडी के खाचों में जकड, बांध, उन्हें बाज़ारों-चौराहों पर भीख मांगने छोड दिया जाता।
जिन भारतीय व्यापारियों के साथ मैं आया उन्होंने गरतोक में तंबू लगा अपनी दुकानें खोल ली थीं। किन्तु मुझे आगे जाना था। तिब्बत में यात्रा के लिए सरकार से सहायता माँगी जा सकती थी। पश्चिमी तिब्बत का गवर्नर, गरपोन, चीनी फौज के डर से गरतोक से राजधानी ल्हासा भाग गया था लेकिन उसका दूसरे नंबर का अधिकारी वहाँ मौजूद था।
अधिकारी एक पत्र देते, जिसे ल्हमिक कहा जाता। उसमें रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के मुखियाओं को आज्ञा दी गई होती कि ल्हमिक-धारक को अगले गाँव तक पहुँचाने के लिए एक तंबू (जो याक के काले बालों का बना होता), सामान ले जाने हेतु एक ख्च्चर या याक, तथा एक पथ प्रदर्शक (रास्ता बताने वाला साथी) दिया जाय। अगले गाँव पहुँचा कर यह प्रदर्शक अपने तंबू तथा याक के साथ लौट जाता और दूसरे गाँव का प्रधान इस काम के लिए अपने लोग उपलब्ध करवाता।
मुझे उत्तर के शहर रुदोक जाना था इसलिए मैं सहायता के लिए उसके पास गया। ल्हमिक देनेवाले अधिकारी ने बताया कि आगे यात्रा करने को संभवतः चीनी फौज से आज्ञा लेनी पडेगी, जो उसी साल 1952 में सिनच्य्यांग प्रदेश से पश्चिमी तिब्बत में आई थी। इसके लिए मुझे चीनी सेना के मुख्यालय, गर-गुंसा, जाना होगा। गर-गुंसा पहुँच मैंने पाया कि चीनी फौज, सतलज नदी किनारे एक सपाट स्थल पर अपना मुख्यालय बना रही थी। उसके सैकडों सैनिक लकडी के खाँचों में रेत-मिट्टी की बडी ईंटें बना धूप में सुखा रहे थे। अचानक मुझे देख वह अचंभे में आ गए। मैं कुछ एक शब्द चीनी भाषा के बोल सकता था, जिसे मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीखा था। मैंने बताया कि मैं भारत से आया हूँ और उत्तर, चीन की ओर, यात्रा करना चाहता हूँ।
उन दिनों तिब्बत में चीनी सेना के प्रवेश के कारण चीन-भारत संबंध अच्छे नहीं थे। एक भारतीय को अपने खेमे में पा चीनी सैनिक हक्के-बक्के थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे उससे कैसा व्यवहार करें? उन्होंने मेरे अचानक आने की खबर और आगे यात्रा करने की इच्छा अपने सिनच्यांग या संभवतः बेजिंग के उच्च अधिकारियों को फैसला लेने भेजी हो! चीनी सैनिकों के पास दो सिपाहियों द्वारा हाथ से घुमा कर बिजली पैदा करने का डाइनमो (यंत्र) था। उसकी बिजली से संकेतों द्वारा समाचार भेजने की एक मशीन भी थी। मुझे रुकने को कहा गया। मैं एक खच्चर पर अपने खाने-पीने का सामान ले कर भारत से आया था। अंधेरा घिरने लगा तो मुझे पास ही एक छोटे से मठ में रहने ले जाया गया। मैंने देखा कि उस मठ की सपाट छ्त पर एक मशीनगन लिए सैनिक बैठा था और मुझे हिदायत दी गई थी कि पेशाब या नदी में हाथ-पैर धोने दूर न जाऊँ।
दूसरे दिन कार्यालय ले जाकर मुझसे पूछताछ शुरू हुई। क्या नाम है? कहाँ रहता हूँ? क्या करता हूँ? क्यों और कैसे तिब्बत आया? किस रास्ते? किसके साथ? इत्यादि। मुझे इतनी चीनी भाषा नहीं आती कि सब सवाल समझ सकूँ और उत्तर दे सकूँ। इसका समाधान करने कुछ अंग्रज़ी-जाननेवाला चीनी दुभाशिया बुलाया गया। उसके आने पर सवालों की झडी लग गई। जवाब दुभाशिया नोट करता और आगे कहीं भेजता। दूसरे दिन नए सवाल आते – समाचार पत्र में क्या काम करता हूँ? समाचार पत्र सरकारी, निजी कंपनी या व्यक्ति विशेष का है? चीन तथा तिब्बत के बारे में समाचार पत्र क्या लिखता है? उसका संपादक कौन है? समाचार पत्र कहाँ-कहाँ बिकता है? इत्यादि। यह पूछताछ कई दिनों चली। प्रतिदिन नए सवाल, दूर किसी पूछनेवाले से आते और उनका उत्तर मुझसे जानकारी ले, भेजा जाता। मुझे बताया नहीं गया कि मैं आगे जा सकता हूँ कि नहीं?
मेरा खाने का सामान कुछ समय बाद समाप्त होने लगा था। यह देख चीनी अधिकारी मुझे अपने नए बने मुख्यालय में रहने ले गए। सिपाही दिनभर मिट्टी-रेत की ईंटें बनाते, दीवारें खडी करते, वौली-बौल खेलते और शाम को सामूहिक गीत गाते। मैं भी गाने वालों के साथ बिठाया जाता. उनके कई गीत मुझे याद हो चले थे। एक गीत जो मुझे अभी भी याद है –
तुंग फांग हुंग, थै यांग सिंग.
चुंको छ ल्यगो माउज़े तुंग!
(आकाश में लालिमा छाई है, सुबह होने को है. चीन में हमारे अपने मउज़े तुंग हैं)
अब चीनियों की रसद भी समाप्त होने लगी थी। उनका रसद भंडार लगभग महीने-भर यात्रा की दूरी पर, बर्फ-ढंके ऊँचे क्यूनलुन पर्वत पार सिनच्यांग प्रांत में था। तब चीनी फौज ने कुछ शिकारी इधर-उधर भेजने शुरू किए जो जंगली गधों तथा याकों को मार लाते और उनका मांस पका चावल या मांड के साथ अपने सिपाहियों को खाने को देते। पास बहती सतलज नदी मछलियों से भरी थी किन्तु अधिकांश तिब्ब्ती मछली नहीं खाते। चीनी फौज ने सिपाही भेज मछली पकडने का अभियान आरंभ किया। उनको पकड, रस्सियों पर टांग, धूप में सुखा उनके ढेर लगाए जाने लगे और खाने में सूखी मछली मिलने लगी। सिपाही कभी बड़े जंगली याक भी मार लाते।
सितंबर में ऊँचे पहाडों पर बर्फ पड़ने लगी और भारत लौटने के रास्ते बंद होने लगे थे। भारतीय व्यापारी ऊन, नमक, सुहागा, इत्यादि लाद वापस जाने लगे। तब भी मेरे बारे में कोई फैसला नहीं आया। मैं अब तक चीनियों के पास दो महीने से अधिक रह चुका था। मुझसे पूछ-ताछ के बाद शायद यह स्पष्ट हो चला था कि मैं जासूस नहीं हूँ। अब कुछ शब्दों तथा इशारों से चीनी सैनिकों से बातचीत हो जाती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कई चीनी सिपाही मैक्सिम गोर्की की लिखी पुस्तकें पढ़ चुके थे।
एक दिन अचानक बताया गया कि मुझे भारत वापस लौटने की आज्ञा मिल गई है। सैकडों मील पैदल चल मेरे जूते फट कर बुरी हालत में थे। चीनी फौज तब कैनवास (रबड तले और ऊपर कपडे के) जूते पहनती थी। उनके गोदाम में मेरे लिए एक जोड़ी तलाशी गई। भारत आने लिए 16,000 फीट ऊँचाई में एक ही पास लीपू लेख खुला था। लीपू लेख पार कर मैं एक जंगल से होता हुआ भारत की पहली बस्ती जिप्ती पहुँचा। वहाँ से 30 मील प्रति दिन चलकर पाँच दिन में काठगोदाम रेल स्टेशन आया, जहाँ से दिल्ली के लिए रेल पकड़ी।
सारी दुनिया में अब तक शोर मच चुका था कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया है। कोई भी संवाददाता तब तक तिब्बत नहीं गया था। दिल्ली पहुँच सीधे देवदासजी के पास गया। मुझे देख देवदासजी बोले इतने समय से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई! हम तो समझे तुम वहाँ मर गए हो! उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ, कहाँ-कहाँ रहे और क्या देखा?

पहाड़ ऑनलाइन का सम्पादन, पहाड़ से जुड़े सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह करता है। इस उद्देश्य के साथ कि पहाड़ संबंधी विमर्शों को हम कुछ ठोस रूप भी दे सकें।