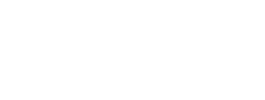जो मरा मुठभेड़ में उस नक्सली को कब तलक
क़ातिल-ओ-रहज़न कहेंगी पंक्तियां अखबार की?
माल रोड पर टहलते हुए मैंने गिरदा को ताज़ा लिखा शेर सुनाया। उन दिनों गिरदा हमारे हर कच्चे-पक्के में ‘संभावना’ तलाश लेते थे और इससे हमें बार बार “इस्लाह-ए-उस्तादाँ” ले लिए उनके पास जाने का हौसला मिलता था।
“यार भुली लिखा तो अच्छा है तूने। बस पंक्तियाँ की जगह सुर्खियाँ लिख कर देख तो?”
जो मरा मुठभेड़ में उस नक्सली को कब तलक
क़ातिल-ओ-रहज़न कहेंगी सुर्खियां अखबार की?
देख आ गया न वज़न शेर में?”, गिरदा ने मुझे चकित करते हुए अपनी बात पूरी की।
मैं और गिरदा कई बार साथ-साथ टहलते हुए तल्ली से मल्ली जाते थे। टेलीफोनएक्सचेंज के सामने गिरदा, राजा बाबू और पिरम के सामूहिक और सार्वजनिक ओड्यार तक पहुँचते पहुंचते राजनीति, संस्कृति, अपसंस्कृति, कविता, क्रांति और बदलाव जैसे कई मुद्दों पर हम गिरदा की थाह लेते थे।
मैंने उन्हें सबसे पहले देवसिंह बिष्ट संघटक महाविद्यालय में आयोजित एक कविता गोष्ठी में देखा था और उनकी करुणा भरी आँखें ताउम्र मेरी स्मृति में अंकित हो गईं। मोटे खद्दर का पाजामा, कुर्ता और भोटी। कंधे पर काग़ज़-पत्तरों और कविताओं से भरा झोला, काले लंबे बाल, चार-पाँच दिन से उग आई दाढ़ी के खूँट, लापरवाह-बेपरवाह चाल, नम्रता से सब परिचित-अपरिचितों के सामने झुकता सिर, नमस्कार में उठे हुए हाथ और हाव-भाव में ऐसा गँवईपन कि आभिजात्य भद्रलोक को कुंठित कर डाले।
नैनीताल मेरी नज़रों में आभिजात्य लोगों का ही शहर तो था। यूरोपीय ठसक वाला, अँग्रेज़ी के माहौल में डूबता-उतराता शहर जहाँ रविवार को स्टिक लिए हुए लोग गिरजाघर जाते दिखते थे। तराई के ऊँघते हुए क़स्बे किच्छा में जब हम टेरीकॉट की पैंट-क़मीज़ को फ़ैशन स्टेटमेंट मानते थे और ‘हैलो’ कहने वाली लड़कियों के चाल-चरित्र पर संदेह करने लगते थे, जब डार्लिंग शब्द हमारे लिए अश्लील हुआ करता था क्योंकि उसे फ़ल्मी विलेन अजित अपने हरम की मोना को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया करता था, जब रुद्रपुर डिग्री कॉलेज की लड़कियाँ अपने होने पर अफ़सोस जताती और सकुचाती हुई सी सलवार-कमीज़ पहने पढ़ने चली आती थीं और हमारा उनके लिए और (अफ़सोस) उनका हमारे लिए जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब नैनीताल के लड़के लड़कियाँ जिस वक़्त डेनिम्स की जींस-जैकेट में एक दूसरे को मुस्कुराते हुए ‘सो, हाउआय्यू?’ कहते दिखते थे मैं अपनी टेरीकॉट की पैंट-शर्ट सहित ज़मीन में दस फ़ुट नीचे धँस जाना चाहता था। डीएसबी में एडमिशन लेने के बाद ऐसे गाढ़े अँग्रेज़ी माहौल में मुझे ठेठ पहाड़ी जुमले ‘भभरि जाने’ का असली एहसास होने लगा।
और तब गिरदा प्रकट हुए।
“ये गिरीश तिवाड़ी हैं। गिरदा। आज इनसे इंटरनेशनल गाने को कहेंगे”, मेरे हॉस्टल के परिचित और दोस्त प्रदीप तिवाड़ी ने मेरे कान में गिरदा का परिचय दिया। यहाँ ऐसे ‘हैलो-हाय’ वाले माहौल में कौन है ये जो ‘इंटरनेशनल’ गाएगा – मैं सोचने लगा। पर उस दिन गिरदा ने इंटरनेशनल नहीं गाया बल्कि अपनी एक कविता सुनाई – कितना करती है सरकार लोगों के लिए!
उस साल सरकार ने कड़कती ठंड में नैनीताल के चौराहों पर लोगों के लिए अलाव का प्रबंध किया था और गिरदा ने सरकार का एहसान चुकाने के लिए ये कविता लिखी थी:
इस साल पूष माह
शहर नैनीताल में
दो एक दिन से,
दो एक दिन तक
सरकारी आग मुफ़्त है।
हर तिराहे चौराहे पर
लोग कह रहे हैं,
कितना सोचती है सरकार
लोगों के लिए!
अगले ही साल शरदोत्सव के दौरान पुलिस की गोली से मल्लीताल में एक अनाम चूरन वाला मारा गया। गिरदा ने फिर लिखा:
गोलियाँ कोई निशाना साधकर दाग़ी थीं क्या?
ख़ुद निशाने पर पड़ी आ खोपड़ी तो क्या करें?
गिरदा हमारी पाठशाला थे और वो ख़ुद समाज की पाठशाला में पढ़े थे। उनके लोहे को मार्क्सवाद और वामपंथी विचारधारा ने जो धार दी दरअसल वो लोहा उनके अपने अनुभव से ढाला गया था। अपनी कविताओं और गीतों के ज़रिए गिरदा ने हमारी पीढ़ी के कई लोगों को अन्याय के ख़िलाफ़ क्रोधित होना और क्रोध को प्रकट करने की अहमियत बताई।
उन्होंने हमें गौर्दा, अदम गोंडवी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अली सरदार जाफ़री, नाजिम हिकमत, अर्नेस्तो कार्देनाल जैसे कई लोगों का नाम लेने की तमीज़ सिखाई, उनकी कविताओं/गीतों को समझना सिखाया और ये सिखाया कि इनके लिखने का मक़सद सिर्फ़ लिखना ही नहीं था। नैनीताल और अल्मोड़ा की सड़कों पर जुलूस के आगे आगे चलते हुए दाहिने हाथ की एक थाप एक बार हुड़के पर और दूसरे बार माथे पर आ गए पसीने को पोंछते हुए वो गाते थे:
किसके माथे से ग़ुलामी की सियाही छूटी, कौन आज़ाद हुआ…कौन आज़ाद हुआ।
या
सौ में सत्तर आदमी फ़िलहाल जब नाशाद है,
दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है?
अब नई पीढ़ी पे मबनी है वही जजमेंट दे,
फ़लसफ़ा गाँधी का मौजूँ है कि नक्सलवाद है.
या गौर्दा की कविताओं को नए तेवर देते हुए जंगल के दुश्मनों को चुनौती देते थे:
अब तुम हमरी लीलामी के करला,
अब करुलों हम तुमरो हलाल…..
हलाल कहते हुए वो अपने हाथ को आरे की तरह चलाते थे और उनके चेहरे पर आततायी को सज़ा देने के बाद आने वाला संतुष्टि का भाव होता था। पर यही गिरदा पहाड़ की सुंदर शामों का उत्सव मनाते भरपूर श्रृंगार में डूबकर गाते थे: डानकाना सिंदूर फोकि गो… राजुला शौक्याणि जसि हुलरि ऐगे ब्याल… हुलरि ऐगे ब्याल…. तो। फिर वो बताते थे कि क्यों फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ उनके महबूब शायर हैं – “क्योंकि उस आदमी ने हमें लड़ने के साथ साथ मुहब्बत करना भी सिखाया”।
फिर अचानक एक के बाद एक कई बदलाव हुए। अब ये याद नहीं कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में पर इतना ज़रूर याद है कि इन बदलावों की शुरूआत के कई बरसों बाद उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नाम से ‘संघर्ष’ जैसा अड़चनी शब्द हटा कर ‘लोक’ जैसा न्यूट्रल शब्द डाल दिया गया। उत्तराखंड लोक वाहिनी का नाम उस दौर में बदला जब उत्तराखंड में एनजीओ ने टिड्डीदल की तरह उतरना शुरू किया था। गाँव-गाँव, क़स्बे-क़स्बे, शहर-शहर में ड्रॉपआउट कम्युनिस्ट और आंदोलनकारी अपना इनक़लाबी बाना पहने रहने की ग़लतफ़हमी पाले हुए एनजीओ खोलने के लिए फॉर्म भरने में लग गए।
उस दौर में हमें पहाड़ में एडवोकेसी, ग्रासरूट्स, एमपावरमेंट जैसे कई नए शब्द सुनाई देने लगे थे। साथ ही हमारे कई साथी अब ‘समाज परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं’ कहने की बजाए कहने लगे थे – “हम महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं।”
ये नई चीज़ें सिर्फ़ पहाड़ में लाए जा रहे बड़े बदलाव की ओर इशारा ही नहीं कर रही थीं बल्कि ग़रीबों के पक्ष में खड़े हो रहे नौजवानों, कवियों, लेखकों और नाट्यकर्मियों के नज़रिए में धीरे धीरे आ रहे बदलाव की झलक भी दे रही थीं। ये कुछ कुछ नई उम्मीदें जगाने वाला मगर साथ ही ढेर सारी पस्तहिम्मती देने वाला दौर था। सुरा शराब विरोधी आंदोलन ने उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों, ठेकेदार और दलाल टाइप लोगों को नकार कर उसकी जगह एक नई जागृति और नई राजनीति का भरोसा जगाया था। चिपको आंदोलन की वामपंथी धारा से निकले डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट, पीसी तिवारी और प्रदीप टम्टा (बिलकुल वही प्रदीप टम्टा जो रामविलास पासवान की दलित सेना में करियर ढूँढते हुए बरास्ता बहिन मायावती काँग्रेस पार्टी की उसी सोनिया गाँधी और उसी हरीश रावत के शरणागत हुए जिनकी राजनीति के ख़िलाफ़ कमर कसते मैंने उन्हें कई बार अपनी किशोर वय में देखा था) जैसे नौजवान तब उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में थे और शेखर पाठक या नाट्यकर्मी ज़हूर आलम या उससे गहरे तौर पर जुड़े हुए थे।
और इन सब ‘राजनीतिक’ लोगों को लोक से जोड़े रखने और दरअसल लोक परंपराओं से ही प्रेरणा लेते रहने की याद दिलाने का काम करते थे गिरीश तिवाड़ी ‘गिरदा’।
उस दिन डीएसबी में गिरदा को देखने के कुछ दिन बाद इस टीम के लोगों को मैंने एक साथ ‘नैनीताल समाचार’ के तल्लीताल वाले दफ़्तर में इकट्ठा पाया। राजीव लोचन साह, गिरदा, गोविंद पंत ‘राजू’ आदि के साथ साथ हमारे नैशनल मूवमेंट पढ़ाने वाले ‘सर’ यानी शेखर पाठक भी ‘समाचार’ के किसी विशेषांक के संपादन में हाथ बँटाने वहाँ आए थे। बाद में पता चला कि वो जगह उन सबका रोज़ाना का अड्डा भी था। उन्हीं दिनों ‘पहाड़’ पत्रिका के पहले अंक के प्रकाशन की तैयारियाँ भी चल रही थीं। इसी अड्डे में कुछ महीनों बाद उत्तराखंड के ऐतिहासिक सुरा-शराब विरोधी आंदोलन की रूपरेखा भी उभरने लगी। यहीं (और कई बार उमा भट्ट व शेखर पाठक के घर पर) बैठकें होने लगीं, पोस्टर और पर्चे बनाए जाने लगे, आंदोलन के विरोधियों का जवाब देने के लिए तर्क तैयार किए गए और शराब माफ़िया को शह देने वाले प्रशासन के ख़िलाफ़ बेख़ौफ़ खड़े होने के संकल्प लिए गए।
पर बिना राजनीतिक दिशा के ये आंदोलन आख़िर जाएगा कहाँ? क्या हमने अपनी राजनीति के बारे में कोई साफ़ समझ बनाई भी है? आंदोलनकारियों के बीच से ही गाहे-बगाहे ऐसे सवाल भी उठे और उनके जवाब भी अपनी तरह से देने की कोशिशें हुईं – राजनीति जनता के बीच से ही पैदा होती है, कोई आसमान से नहीं टपकती। जनता अपनी राजनीति ख़ुद तय कर लेगी।
मास्टर और शिष्य के बीच की दूरी पाटना तब हमारे लिए संभव नहीं था इसलिए शेखर पाठक हमारी पहुँच से दूर ही रहे या कहें कि उनसे एक ऐसा रिश्ता हमने ही बना लिया था। बचे गिरदा जो सहज उपलब्ध थे और अपने राजनीतिक सवालों को लेकर हमने उनकी ओर ताकना शुरू कर दिया। “गिरदा, पीसी पांडे तो कहते हैं कि ये सुधारवादी आंदोलन है और ऐसे आंदोलनों के बारे में मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मेनीफ़ेस्टो में बहुत पहले लिख दिया है कि ये स्टेटस-को की ताक़तें हैं? लेनिन ने भी तो कहा था कि बिना कम्युनिस्ट पार्टी के क्रांति संभव नहीं है. तो फिर शराबबंदी जैसे सुधार करने से समाज कैसे बदलेगा?”
अगर ऐसे सवालों से गिरदा को कोफ़्त होती भी रही होगी (और होती ज़रूर होगी) तो उन्होंने ये हम पर कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया। अपने ओड्यार में पानी भरे डेग से छोटे छोटे आलू निकाल कर छीलते हुए वो आज़िज़ आकर आख़िर कही देते थे – यार भुली मैं तो ठैरा कल्चरल फ्रंट का आदमी, राजनीतिक सवाल तो शमशेर और पूरन (पीसी तिवारी) को हल करने होंगे।
अपने कल्चरल फ़्रंट का आदमी होने का स्थूल सबूत देने के लिए वो आलू की परात एक किनारे करके हारमोनियम खींच लेते और फिर शुरू होता फ़ैज़ से लेकर अदम तक की इनक़लाबी ग़ज़लों और नज़मों का सिलसिला। राजनीतिक सवालों के पचड़े में न गिरदा कभी पड़े और शायद न ही उन्होंने विचारधारा को कभी अपने गले की फाँस बनने दिया। फिर भी गिरिश तिवाड़ी ‘गिरदा’ एक घोर राजनीतिक व्यक्ति थे और वो अपनी विचारधारा के प्रति हमेशा ईमानदार बने रहे।
भारत में पहले नव-जनवादी क्रांति होनी चाहिए या सोवियत-स्टाइल में सामूहिक विद्रोह की अपील की जानी चाहिए? क्या गाँवों से शहरों को घेरना सही रणनीति है या पहले शहरी सर्वहारा मज़दूर को गोलबंद किया जाना ज़रूरी है? शायद इन सवालों ने उन्हें ज़्यादा परेशान कभी नहीं किया। उनकी कविता ग़रीब के राज के ज़रिए सामाजिक समता का सपना देखती और दिखाती थी (और अब भी दिखाती है), पर ग़रीब का राज आएगा कैसे ये शमशेर और पीसी जानें।
सुरा-शराब विरोधी आंदोलन का आख़िर वही हुआ जो सरकारें ऐसे आंदोलनों का करती हैं। शराबबंदी की कुछ घोषणाएँ की गईं। कुछ समय तक इन घोषणाओं पर अमल भी हुआ पर बाद में राजस्व कमाने के नाम पर एक बार फिर से शराब के ठेकों की नीलामी हुई और ठेकेदारों की बन आई। पर आंदोलन के हुलार पर उतरने के साथ ही संगठन के सामने पुराना सवाल फिर आ खड़ा हुआ – उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी की राजनीतिक दिशा क्या होगी?
संगठन और उससे जुड़े हुए लोग इस सवाल से अलग अलग, अपने अपने तरीक़े से जूझ रहे थे। इस बीच इंडियन पीपुल्स फ़्रंट के ज़रिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी – मार्क्सवादी-लेनिनवादी (लिबरेशन) ने वाहिनी में ‘तपे-तपाए राजनैतिक रूप से सजग’ कैडरों की संभावना देखते हुए उसमें अपनी पैठ बनानी शुरू की जिसका अंत वाहिनी में टूट-फूट, बिखराव और कड़वाहट में हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा असर हुआ वाहिनी से जुड़े कई नौजवानों पर जो कम्युनिस्ट पार्टी और विचारधारा के मंतव्यों पर ही शक करने लगे।
शमशेर सिंह बिष्ट ने इन स्थितियों के लिए लिबरेशन और आइपीएफ़ की ज़िम्मेदारी को रेखांकित करते हुए उन दिनों स्थानीय अख़बारों में एक लेख भी लिखा था। गिरदा को इस राजनीति पर अफ़सोस ज़रूर हुआ होगा पर वो खांटी राजनीति में पगे लोगों की तरह अंतरसंघर्ष को विकास के लिए ज़रूरी शर्त नहीं मान सकते थे। हो सकता है इन घटनाओं के बाद ही उनका दिल कुछ उचाट भी हो आया हो। जैसा उचाटपन शेखर पाठक के भीतर भी आया प्रतीत होता है और मेरी नज़र में उसी उथल पुथल के बाद बिना उद्घोषणा किए हुए शेखर पाठक ने अपना अलग रास्ता और ‘विचारधाराओं से मुक्त’ राजनीतिक दिशा तय करने का फ़ैसला किया। उसी उथल पुथल के बाद वाहिनी के कई लोग ख़ुद को वामपंथी कहे जाने पर तुरंत सफ़ाई देने की जल्दबाज़ी में दिखाई देने लगे।
ये ‘नशा नहीं रोज़गार दो’ आंदोलन के तिरोहित हो जाने, सोवियत संघ के विखंडित होने के बाद और पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शुरू होने से पहले का वो समय था जब पहाड़ में नई एनजीओ शब्दावली का प्रसार ज़ोर शोर से हो रहा था। गिरदा ने लगभग इसी समय नाट्य-संगीत विभाग से अवकाश ले लिया था और लोगों ने बताया था कि गिरदा अब ‘हिमालयी संस्कृति संस्थान’ नामक एक संग्रहालय के बारे में सोच रहे हैं जिसमें मौसम के हिसाब से हिमालयी लोकजीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
“गिरदा, आप एक इशारा कर देंगे तो कई लोग थैलियों का मुँह खोलने को तैयार हो जाएँगे इस संस्थान के लिए। एनजीओ अपनी फंडिंग देने में भी क़सर नहीं छोड़ेंगे। पर क्या आप ये सब करने को तैयार हैं?” मल्ली ताल की एक चाय की दुकान में बैठकर मैंने गिरदा को उपदेश दे डाला। और गिरदा की सदाशयता कि इसे मेरा बचकानापन कहकर दरकिनार करने की बजाए वो चुप होकर कुछ सोचने लगे। बहुत देर बाद उनके मुँह से निकला: “बात तो ठीक ही कहता है यार तू। अब बता फिर मैं क्या करूँ?” मुझे लगा जैसे गिरदा हार सी मान रहे हों। पर मैं ग़लत था।
बाद में उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें झूँसिया दमाई पर अद्भुत काम करने के लिए कुछ ग्रांट भी मिली। चार-पाँच हज़ार की सरकारी ग्रांट से खुलने वाले रस्तों पर चलकर हमारे कुछ मित्र कालांतर में उत्तराखंड के बड़े एनजीओ मालिक बन गए। गिरदा चाहते तो उनके लिए भी वो रास्ता बहुत आगे तक जा सकता था। अगर वो लोकसंस्कृति की प्रदर्शनी लगाने के प्रोजेक्ट बना बना कर बेचते तो शायद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम और दाम कमा सकते थे। पर उन्होंने ऐसा न करने का फ़ैसला किया।
उस वक़्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अरसे बाद ‘पहाड़’ के पच्चीस बरस पूरे होने के अवसर पर आयोजित किए गए समारोह में भी एक बार यही सवाल सामने आएगा कि ‘पहाड़’ को संस्थागत करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और इस सवाल के जवाब में वहाँ मौजूद उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके एक मुअज़्ज़िज़ सदस्य कहेंगे कि “मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, इन कैन बी अरेंज़्ड।”
यह वाक्य अपने आप में एक युग के अंतर को रेखांकित करने वाला प्रतिनिधि वाक्य था। सन 1983 में पहाड़-1 के विमोचन समारोह में “मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम” कहने वाला ख़ुद को भीड़ के बीच में निर्वस्त्र-सा पाता, पर 25 बरस बाद पिथौरागढ़ में दी गई इस तजवीज़ पर बहस तो हुई मगर भृकुटियाँ नहीं तनीं। हालाँकि इस वाक्य ने मुझे गिरदा के साथ मल्लीताल की चाय की दुकान में हुई उस बातचीत की याद दिला दी थी कि ‘आप चाहेंगे तो थैलियों के मुँह खुल जाएँगे’।
पर सिर्फ़ यही वाक्य बदलाव के संकेत नहीं देता था। ‘पहाड़-1’ के विमोचन के दौरान पिथौरागढ़ के ज़िला परिषद हॉल में जहाँ संपूर्ण बदलाव के जनगीत गाए गए थे, पत्रिका के पच्चीस साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में राजनीति और राजनीतिक सवाल सिरे से नदारद थे – न भाषणों में, न गीतों में और न तेवर में। उसकी जगह स्कूली बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए किए जाने वाले आयोजनों – मसलन स्लाइड शो, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि “रचनात्मक” कार्यक्रमों ने ले ली थी। जहाँ पहले आंदोलनकारी जनसंगठनों की शिरकत ‘पहाड़’ को एक अलग पहचान देते थे, अब सरकार के सचिव और संयुक्त सचिव, सरकार से सहकार की बात करने वाले व्यक्ति और संगठन ‘पहाड़’ की ओर आकृष्ट हो चले थे। चौथे अस्कोट-आराकोट अभियान (2014) में कारपोरेट की शिरकत ने यात्रियों के एक हिस्से को व्यथित किया, हालाँकि आयोजकों का ये कहना भी तार्किक है कि एक खुली यात्रा में शिरकत करना चाह रहे लोगों पर सिर्फ़ इसलिए पाबंदी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो कारपोरेट में काम करते हैं।
इस मायने में ‘पहाड़’ संस्था ने अद्भुत शक्ति दिखाई कि वो, तमाम दबावों के बावजूद, सीधे सीधे एक एनजीओ बनने से अब तक बचा रहा है पर उसमें शुरूआती दिनों से निहित राजनीतिक धार लगभग पूरी तरह बत्थड़ हो गई, या हो जाने दी गई। पर ये भी सच है कि ‘पहाड़’ की संकल्पना किसी राजनीतिक मक़सद को पूरा करने के लिए नहीं की गई थी और न ही वो कभी ‘विचारधारा’-पोषित संस्था रही। ये हिमालय को समझने के लिए बनाई गई संस्था है जिसे शेखर पाठक ने एक लचीला स्वरूप दिया, जिसमें व्यवस्था विरोधी मार्क्सवादियों से लेकर विशुद्ध पर्यावरणवादी और सर्वोदयी-गाँधीवादी विचार वालों को जोड़ा जा सकता था। पर ऐसा भी नहीं हैं कि ‘पहाड़’ विचार या विचारधारा निरपेक्ष संगठन के रूप में जन्मा हो। पहाड़-2 में इसे काफ़ी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है: “इस सामूहिक कोशिश को हम अकादमिक, बौद्धिक एकालाप नहीं बल्कि जनचेतना को प्रखरता देने वाला, पहाड़ के बावत जनता में वैज्ञानिक समझ विकसित करने वाला तथा पहाड़ और उसके पर्यावरण को बचाने वाला कार्यकलाप बनाना चाहते हैं।”
पहाड़ के 25 बरस मनाने के लिए पिथौरागढ़ में हुए समारोह में गिरदा नहीं थे। हमने आधुनिक टेक्नॉलाजी की मदद से नैनीताल में बैठे गिरदा की आवाज़ फ़ोन के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की पर ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पर अगर वो मौजूद होते तो भी क्या हो जाता? क्या विभिन्न तरह के ग्रासरूट संगठनों, सरकारी अधिकारियों, मुझ जैसे कुछ प्रवासियों और कुछ बरायनाम आंदोलनकारियों के बीच घिरा ये जनकवि अब पुरानी ठसक के साथ गा सकता था – अब करुँलो हम तुमरो हलाल? अब तक राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था, गिरदा भी थक चुके थे और बरसों तक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहने के कारण उनकी देह अब जवाब देने लगी थी। पर शराब और बीड़ी फिर भी नहीं छूट पा रही थी।
शराब को ‘रोमैंटिसाइज़’ करने का फ़ैशन पहाड़ में शायद बहुत पहले से रह है। शाम होते ही अधेड़ और बुज़ुर्ग भी शराब का ज़िक्र कुछ ऐसी किशोर-सुलभ शरारत भरी मुस्कान के साथ करते हैं जैसे किसी चीज़ को ज़ाहिर करते हुए छिपाना चाहते हों पर छिपाते हुए ज़ाहिर करने की इच्छा भी हो। पहाड़ के परंपरागत ब्राह्मणवादी समाज में शराब को कभी भी सामाजिक स्वीकार्य उस तरह हासिल नहीं हुआ जैसे यूरोपीय या आदिवासी समाजों में है, या कुछ कायस्थ परिवारों में देखा जाता है। पर इस अस्वीकार के बावजूद शराब का विस्तार पर्वतीय समाज में निर्बाध हुआ है। गिरदा को भी शाम होते ही शराब की हुड़ुक होने लगती थी और आस पास के लोग हँसी-ठट्ठा करते हुए जुगाड़ कर ही दिया करते थे। शराबबंदी आंदोलन के दौरान गिरदा ने अपने मन को मारकर शराब कुछ समय के लिए छोड़ी थी मगर हृदयाघात और तमाम बीमीरियों से घिरने के बाद भी वो इससे अपना पिंड पूरी तरह नहीं छुटा पाए। उलटे उनके जीवन में शराब की अस्वस्थ, ग़लत और ख़तरनाक मौजूदगी जाने-अनजाने उनकी पारिवारिक परंपरा का हिस्सा तक बन गई।
पर शराब पर शायद उन्होंने कुछ लिखा नहीं। या लिखने की हिम्मत नहीं की। शराब की महिमा गाने वाले उर्दू शायर की चिंताएँ कभी उनकी चिंता नहीं बनीं। यानी गिरदा इश्क़ के शायर तो थे मगर शराब के शायर न बन पाए। लगभग उसी तरह जैसे उनकी चिंताओं में ओड़, बारुड़ि, कुल्ली, कभाड़ी तो थे पर वो कभी अपने परिवेश और ‘उच्चवर्ण’ की लक्ष्मणरेखा पार कर दलितों के अपने कवि नहीं बन पाए।
मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि दलित कभी गिरदा की काव्य-चिंताओं में नहीं रहा होगा। अगर उनकी चिंताओं में दलित नहीं होता तो शायद वो फ़ैज़ के कलाम को इतना स्थानीय और इतना ‘पहाड़ी’ अर्थ न दे पाते जैसा उन्होंने दिया। लेकिन गिरदा की राजनीतिक चिंता में दलित एक अलग समूह के रूप में क़तई न आ पाया। उस दौर में ईमानदार जन-राजनीति पर भरोसा रखने वाले वाहिनी के तमाम लोगों (गिरदा और शेखर पाठक सहित) की चिंताओं में दलित ज़रूर था (और आज भी है) पर उसका स्थान वैसे ही था जैसे किसी और शोषित का। वो सब वंचितों के सामूहिक संघर्ष में तो यक़ीन करते थे पर ये कभी न सोच पाए कि उत्तराखंड के 18 प्रतिशत दलितों का यथार्थ दूसरे वंचितों के यथार्थ से अलग भी हो सकता है।
पूर्व कांग्रेसी सांसद प्रदीप टम्टा अब ख़ुद कितने ही बदल गए हों, उनके सवाल अब भी नहीं बदले। वो पूछते हैं – “असकोट-आराकोट अभियान में दलितों की कितनी चिंता झलकती है? क्या इस अभियान के ज़रिए ये जानने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी कि 1974 में दलितों की क्या स्थिति थी और अब 2014 में पहाड़ के दलित कैसे रहते हैं?” ये सवाल आरोप की भाषा में पूछे गए हैं। प्रदीप टम्टा प्रकारांतर से कह रहे हैं कि ब्राह्मण परिवारों में पैदा हुए वाहिनी के प्रमुख लोगों ने दलितों को दूसरी जातियों के वंचितों की कोटि में डालकर उनके साथ होते आ रहे अन्याय का सामान्यीकरण किया है। ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि जैसा सामाजिक तिरस्कार दलित जातियों को झेलना पड़ा वैसा सीमांत में रहने वाले जनजातीय समाज या ‘सवर्ण’ मेहनतकश तबक़े को नहीं। पर क्या इस बात को भुला दिया जाना चाहिए कि शेखर पाठक और शमशेर सिंह बिष्ट ही वो लोग थे जिन्होंने 1980 में सल्ट के कफल्टा गाँव में सवर्णों द्वारा 11 दलितों को ज़िंदा जलाए जाने पर तुरंत वहाँ पहुँच कर दिनमान पत्रिका के ज़रिए उस कांड को दुनिया के सामने रखा। उनकी राजनीतिक सोच में हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा दबे-कुचले और उपेक्षित लोग एक जाति समूह के तौर पर उपस्थित भले ही न रहे हों, पर ये नहीं कहा जा सकता कि दलित समाज शेखर पाठक के रेडार पर कभी आया ही नहीं। ‘पहाड़ -2’ में छपे अपने अकादमिक लेख ‘उत्तराखंड में सामाजिक आंदोलनों का रूपरेखा’ में शेखर पाठक ने लिखा: “आज भी शिक्षा समाज के दलित हिस्सों तक सबसे कम गई है। इसी क्रम में यह वर्ग अन्य सुविधाएँ और साधन नहीं पा सका है और राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्र शक्ति नहीं बन सका है… 1820 में जिन शिल्पकारों को ट्रेल ने परंपरागत दासों और हुक्का छूने या सवर्णों के भोजन स्पर्श करने पर सज़ा पाने वाले समुदाय के तौर पर देखा, वे 150 साल बाद वैसे तो नहीं रह सकते थे, लेकिन स्थिति सामाजिक-आर्थिक संतुलन के उस बिंदु तक नहीं पहुँच सकी, जहाँ कफल्टा जैसी त्रासदी असम्भव हो जाए।”
पर दलित और ग़ैर-जातियों के शोषितों को एक पंक्ति में खड़ा करने की ग़लती वामपंथी रुझान रखने वाले सभी लोगों ने की और दलितों के प्रति भेदभाव न करने को अपनी उदात्तता और प्रगतिशीलता की निशानी के तौर पर हमेशा नुमाया किया। और ये नुमाइश उत्तराखंड आंदोलन के दौरान छलक-छलक कर सामने आई। उत्तराखंड आंदोलन में समाज की कई धाराएँ अपने अपने कारणों से शामिल हुईं। वो एक ऐसा गधेरा बह निकला था जिसमें हिंदूवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी, समाजवादी, साम्यवादी, क्षेत्रवादी, इलाक़ापरस्त, सांस्कृतिक श्रेष्ठतावादी, गाँधीवादी, सर्वोदयी, मातृशक्ति, छात्रशक्ति, सरकारी कर्मचारी आदि न जाने कितनी धाराएँ समाहित थीं। और हाहाकार करते हुए उमड़ चले इस गधेरे को दूर खड़ा होकर तनिक चिंता और तनिक हतप्रभ सा होकर देख रहा था उत्तराखंड का दलित समाज। इस दलित समाज के कानों में वो नारे भी गूँजते थे जिनमें मायावती और काँशीराम की जाति को उछालकर उनका उपहास उड़ाया जाता था। इस आंदोलन में लगभग ललकारने वाली आवाज़ में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को स्थापित करने वाली वो बातें कही जाती रहीं जिन्हें सुनकर पहाड़ का दलित समाज उत्तराखंड आंदोलन से अपना दामन बचाने की कोशिशें करने लगा।
“हमने तो बार बार उनसे कहा है कि जुलूस में शामिल होओ, लेकिन वो आते ही नहीं”, नैनीताल समाचार के दफ़्तर में आंदोलन के उफान के दिनों की एक शाम अख़बार के संपादक राजीव लोचन साह ने मुझसे कहा। कौन थे ये ‘हम’ जो ‘उनको’ बार बार आंदोलन में शामिल होने को कहते थे? और कौन थे वो ‘उनको’ जो इस आंदोलन में शामिल नहीं होना चाहते थे? स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो आंदोलन में शामिल होने की दावत देने वाले वो ‘उच्चवर्णी-उदारवादी’ लोग थे जो उत्तराखंड आंदोलन को सवर्ण जातियों के वर्चस्व से निकालकर सच्चे अर्थों में ‘जन’ आंदोलन बनाना चाह रहे थे। लेकिन वो भी ‘हम’ और ‘वो’ के फ़र्क़ को मिटा नहीं पाए।
मैंने तब इंडियन एक्सप्रेस में उत्तराखंड आंदोलन को मिल रहे अभूतपूर्व समर्थन को ‘सवर्णों की साज़िश’ (अपर कास्ट कंसपिरसी इन उत्तराखंड) बताते हुए एक लेख लिखा था जिसके ज़रिए उन कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की गई थी जिन्होंने पृथक राज्य के आंदोलन को अचानक इतना लोकप्रिय बना दिया। आख़िर क्या कारण था कि सत्तर और अस्सी के दशक में जब जब उत्तराखंड क्रांति दल अलग राज्य की माँग को लेकर कुमाऊँ-गढ़वाल बंद का आह्वान करता था तब तब ये आह्वाहन बुरी तरह फ़ेल हुआ? पहाड़ के प्रभावशाली समुदायों ने पृथक उत्तराखंड की माँग को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का फ़ैसला नहीं किया।
आरक्षण का ऐलान होते ही सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय के छात्र, घरेलू महिलाएँ, अध्यापक और फ़ुटकर आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए और तमाम मंचों से कहा जाने लगा – हमें अपना अलग उत्तराखंड दो, हम अपनी आरक्षण नीति ख़ुद लागू करेंगे। ये सीधे सीधे दलितों और पिछड़ों के ख़िलाफ़ हो रहे ब्राह्मणवादी उभार का नतीजा था।
कुल्ली और कभाड़ियों के पक्षधर गिरदा पृथक उत्तराखंड आंदोलन के इस पक्ष को देखने में शायद फ़ेल रहे और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी, सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता रही। वही नहीं उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के तमाम अगड़ी जातियों के नेता दलितों-पिछड़ों के साथ छिड़े इस द्वंद्व को देखने में असफल रहे। और भी कारण रहे होंगे लेकिन मोटे तौर पर यही वो कारण था कि प्रदीप टम्टा जैसा प्रखर और ओजस्वी छात्र-युवा नेता – जो कभी गिरदा के ओड्यार में उनके, राजा बाबू और पिरम के साथ रहा था – अब धीरे धीरे अपनी जातीय पहचान को पहचानने लगा. मार्क्स और लेनिन के कलैक्टेड वर्क्स की जगह उनकी अलमारी में आंबेडकर ग्रंथावली सजने लगी।
आंबेडकर थे कहाँ गिरदा की या उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के दूसरे नेताओं की चिंताओं में? और आज भी कहाँ हैं? ये सवाल प्रदीप टम्टा उठाते हैं, हालाँकि ये वही बेहतर जानते हैं कि काँग्रेस जैसी घोर यथास्थितिवादी पार्टी के सांसद हो जाने, उत्तराखंड के प्रमुख काँग्रेसी नेताओं में गिने जाने और मुख्यमंत्री हरीश रावत के सिपाहसालार बन जाने के बाद वो ख़ुद कितना ऐसे सवाल उठाने लायक़ बचे हैं। लेकिन उनके उदाहरण से उपजा ये सवाल अब भी मुँह बाए खड़ा है कि कुल्ली-कभाड़ियों की चिंता करने वाला कवि क्यों अपने सबसे क़रीब रहने वाले दलित नौजवान को अपनी राजनीति और संस्कृतिकर्म से जोड़कर नहीं रख पाया? झूँसिया दमाई और सूरदास जैसे नगीनों के पारखी क्यों प्रदीप टम्टा और उस तिरस्कृत समाज को नहीं परख सके, उनकी दलित संबंधी चिंताओं को क्यों अपनी राजनीति के ज़रिए नहीं उठा पाए? क्या गिरदा और समाज परिवर्तन की ईमानदार लड़ाई लड़ने वाले दूसरे लोगों की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी कि गाँव से बाहर रहने वाले शिल्पकारों को इतना भरोसा दिलाते कि वो पृथक राज्य की लड़ाई से जुड़ने की हिम्मत जुटा पाते?
गिरीश तिवाड़ी ‘गिरदा’ अगर ज़िंदा होते तो….
मैं उनसे ज़रूर पूछता कि ‘तुमने हमें फ़ैज़ और अदम की दुनिया में दाख़िला तो दिलवाया पर ख़ुद ज्योतिबा फुले और भीमराव आंबेडकर के टोले में जाने की ज़हमत क्यों नहीं उठाई, गिरदा’?
और जैसे ही मैं लेख समाप्त कर रहा था कि गिरदा के एक हमनवा अचानक जैसे दशकों पुरानी समय की किन्हीं रहस्यमयी परतों को उघाड़ते हुए चले आए और मुलायमियत से कान खींचते हुए मुस्कुरा कर पूछने लगे – हमें क्यों भूल रहे हो? ये हैं वैद्यनाथ मिसिर जिन्हें हम प्यार से बाबा नागार्जुन पुकारते थे। किताबों की अलमारी से संदर्भ के लिए मैंने बरसों से सहेज कर रखा पहाड़ -2 का अंक निकाला और उसके पन्ने पलटते हुए मुझे नज़र आया पूरी तरह पीला पड़ चुका काग़ज़ का एक टुकड़ा जिसमें 15 सितंबर 1983 को बाबा ने मुझे अपनी एक कविता का अंतिम अंश लिखकर दिया था। बाबा नागार्जुन को शेखर पाठक ने उसी दौर में नैनीताल आमंत्रित किया था जिसका ज़िक्र इस आलेख में किया गया है। मैं बरसों तक इस काग़ज़ को ढूँढता रहा था पर इसे आज गिरदा को श्रद्धांजलि देते समय ही मिलना था. शायद इन पंक्तियों के बिना गिरदा को श्रद्धांजलि पूरी भी नहीं होती:
“उत्तराखंड में
मिल रही हैं मुझे
ठौर-ठौर पर
जुझारू टीम
तरुणों-तरुणियों की…
यही हमारे सही वंशधर हैं
मैं बेहिचक सौंप सकता हूँ
इन्हें अपनी शेष आस्था…
(एक कविता का अंतिम अंश)
– नागार्जुन 15.9.83.”
पर बाबा इस कविता में किस तरह के जुझारूपन की बात कह रहे हैं? उनकी कौन सी ऐसी ‘शेष आस्था’ थी जिसे वो उत्तराखंड के तरुणों-तरुणियों को बेहिचक सौंपना चाहते थे? क्या वो सरकार और हुक्मरानों के साथ क़दमताल करने की आस्था थी? क्या वो सरकार के साथ सहकार करने की आस्था थी?
इन सवालों का जवाब उत्तराखंड की जुझारू टीमें ही दे पाएँगी।

पहाड़ ऑनलाइन का सम्पादन, पहाड़ से जुड़े सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह करता है। इस उद्देश्य के साथ कि पहाड़ संबंधी विमर्शों को हम कुछ ठोस रूप भी दे सकें।