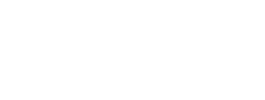सुन्दरलाल बहुगुणा (9 जनवरी 1927, ग्राम मरोड़ा, टिहरी-21 मई 2021, ऋषिकेश) का जीवन एक लम्बी यात्रा है, कश्मीर से कोहिमा की तरह। उनका जाना एक ऐसे जटिल युग का अन्त है जो औपनिवेशिक तथा रियासती शासकों से लड़ते परतंत्र भारत में शुरू होता है और जिसका अन्त कोरोना के निर्मम दौर और भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्दयी और निर्लज्ज होने के मध्य हुआ। जब वे धरा में आये तो टिहरी रियासत में दमन और हत्याकांड हो रहे थे और शेष भारत में भी। जब वे गये तो देश को बेच रहे सत्ताधारी अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं। वोट के लिये इस्तेमाल होती रही जीवनदायिनी गंगा कई स्थानों पर लाशों से पटी है और यमुना तथा नर्मदा नदियां भी। सत्ता विश्व इतिहास के सबसे बड़े झूठ लगातार बोल रही है।
यह युग टिहरी रियासत में चला और उसके बाहर भी। यह एक बालक के विकसित होने, सुमन का साथी बनने तथा आजादी का आकांक्षी बनने की कहानी है। प्रजामंडली और राजनैतिक कार्यकर्ता बनने की। फिर यह एक दम्पति के बनने और विकसित होने की कहानी है। वे समाज को कैसे बनाते हैं और समाज उन्हें कैसा बनाता है यह पक्ष भी इस कहानी से जुड़ा है। ऐतिहासिक शक्तियाँ किसी या किन्हीं लोगों से क्या क्या काम कराती हैं, यह देखना भी कम रोचक नहीं।
विद्रोही नई पीढ़ी
टिहरी शहर से 5-6 किमी. दूर मरोड़ा गाँव सुन्दरलाल का जन्म मां पूर्णा देवी और पिता अम्बादत्त के घर हुआ। पिता टिहरी रियासत के वन कर्मचारी थे, जैसे करीब के गांव मालदेवल की विमला (4 अप्रैल, 1932) के पिता नारायण दत्त नौटियाल भी। दोनों लगातार दौरों में रहते थे। मालदेवल में भी मां रत्नकान्ता परिवार को संभालती थी। इन घरों में राज विद्रोही पैदा हो रहे थे। सुन्दरलाल तो अकेले विद्रोही थे पर नारायण दत्त नौटियाल की चार सन्तानें विद्रोही बनी। दोनों बेटियों – कमला और विमला – ने सरला बहिन के लक्ष्मी आश्रम विद्यालय में सामाजिक कर्मी बनना सीखा। तीसरी बहिन उर्मिला भी वहीं दीक्षित हुईं। दोनों भाई बुद्धिसागर और विद्या सागर पहले प्रजामण्डली और फिर क्रमशः कांग्रेसी और साम्यवादी बने। फिर आजन्म लड़ाकू बने रहे। विद्या सागर सुप्रसि़द्ध साहित्यकार बने। विधायक भी। साम्यवादी पार्टी ने उन्हें कुछ समय के लिये टिहरी बांध का विरोध करने के कारण पार्टी से निकाला था। बुद्धिसागर संग्रामी और हिमाचली बन गये। उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था।
मरोड़ा और मालीदेवल भागीरथी किनारे के गांव थे। पीने का पानी भागीरथी से लाया जाता था। गंगा नाम इसीलिये यहां बहुत प्रचलन में था। सुन्दरलाल को भी पहला नाम गंगाराम मिला था, अपनी एक बुआ की तरह ही। भागीरथी इस समाज के चेतन-अवचेतन में उसी तरह बसी थी, जैसे हिमालय की पहली बसासतों से गंगासागर तक या कोई भी और नदी अपने किनारों के समाजों में।
प्रारम्भिक शिक्षा इन्टर तक प्रताप इन्टर कालेज, टिहरी में हुई। वहीं उन्होंने पहली बार श्रीदेव सुमन को देखा था। दोनों की उम्र में 11 साल का फर्क था और चम्बा की धार के आरपार दोनों के गाँव थे। आगे की पढ़ाई तक भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू हो गया था। वह टिहरी और मसूरी में सुमन के साथ काम करने लगे थे। 1930 के रवाँई हत्याकांड के बाद रियासत में चुप्पी थी। राजा यूरोप में घूम रहा था और कर्मचारी दमन में जुटे थे। 1939 में देहरादून में गठित प्रजामण्डल को ‘राजा की छत्रछाया स्वीकार करने‘ के बाद भी रियासत के भीतर काम नहीं करने दिया जा रहा था। 1942 में एक दिन सुन्दरलाल की मां पानी लाने भागीरथी तक उतरी तो बरसात से आक्रामक बनी नदी उन्हें बहा ले गई। वे 15 साल के थे। इसी बीच सुमन की गिरफ्तारी के बाद जेल में यातनाओं का दौर चल रहा था। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद सुमन ने प्राण त्याग दिये।
सुमन के जेल जीवन की खबरें सुन्दरलाल अखबारों में भेज देते थे। रियासत की पुलिस तथा खुफिया विभाग को बालक पर शक हुआ और गिरफ्तारी हो गई। एक फोड़े के कारण अस्पताल ले जाने के बहाने बाहर आ सके और फिर जेल ले जाये जाने से पहले लाहौर भाग गये। 1945 का साल शुरू हो चुका था। सुन्दरलाल ने सनातन धर्म कालेज, लाहौर में बी.ए. में प्रवेश ले लिया था। बड़े भाई वहीं पढ़ रहे थे। विश्वयुद्ध समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता सेनानी जेल से बाहर आ रहे थे। टिहरी में सुमन की शहादत के बाद की चुप्पी शीघ्र टूटने वाली थी। सुमन की शहादत ने टिहरी में प्रजामण्डल को जीवन दिया। लाहौर में प्रवासी गढ़वालियों ने प्रजामण्डल की शाखा खोली थी, जिसमें सुन्दरलाल जाने लगे थे। एक दिन रियासत की पुलिस की सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस उनकी खोज में आई।
सुन्दरलाल को भूमिगत हो सरदार मानसिंह का रूप लेना पड़ा। कुछ समय बाद भागकर वह लायलपुर में रहे। वहां एक साम्यवादी सरदार जी ने उन्हें प्रिन्स क्रोपोटकिन की किताब पढ़ाई। दूसरे सरदार जी ने अपने बच्चे को पढ़ाने का काम दे दिया। गुरूमुखी सीखी। गुरुग्रन्थ साहिब और गांधी की रचनायें पढ़ी। लाहौर लौट कर फिर पढ़ाई शुरू की। इस समय तक विभाजन की दुखद कहानी शुरू हो चुकी थी। इम्तहान देकर सुन्दरलाल जून 1947 में टिहरी आ गये। प्रथम श्रेणी में बी.ए. किया और टिहरी में प्रजामण्डल के कार्यो में जुट गये। 15 अगस्त 1947 का स्वागत उन्होंने टिहरी में किया। 1948 में प्रजामण्डल की ओर से राज्य की विधान सभा का चुनाव लड़े और हार गये। 21 साल के तरुण के जीवन का यह पहला और आखिरी चुनाव था।
सुन्दरलाल को टिहरी के कांग्रेस जिला सचिव का दायित्व सौपा गया। 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया और प्रजामंडल का कांग्रेस में। इसी साल विमला नौटियाल अध्ययन के लिये सरला बहन के विद्यालय में कौसानी गई। स्थानीय अखबार में इसका विज्ञापन भाई बुद्धिसागर ने देखा था और बहन को वहां जाने के लिये प्रोत्साहित किया था। अब तक प्रजामण्डल का विलय कांग्रेस में हो चुका था। 1950 में सुन्दरलाल ने जन सहयोग से पहला काम टिहरी में ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना का किया। यह दलित समुदाय और समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का एक आधार शिविर सा बना। हरिजन सेवक संघ की ओर से काम हो रहे थे। टिहरी में जनगायक गुणानन्द पथिक तब ‘गांधी जी का प्यारा हरिजन’ जैसा गीत गा रहे थे। तभी यह समाज दलितों के मंदिर प्रवेश की सफल लड़ाई भी लड़ा। जब मीरा बहन भिलंगना के गेवली गांव में ‘गोपाल आश्रम’ बना कर रहने लगीं तो सुन्दरलाल उनसे मिले और ग्रामविकास पर चर्चा की। वन सम्बंधी प्रारम्भिक चेतना जहां रियासत के वन आन्दोलनों से बनी थी, वहीं पारिस्थितिकी का पक्ष मीरा बहन के सम्पर्क में आने से विकसित हुआ। अध्ययनशीलता ने भी युवा सुन्दरलाल का जंगलात ज्ञान बढ़ाया।
दृश्य का बदलना
1956 में नारायण दत्त ने बेटी विमला का विवाह सुन्दरलाल से तय किया। सरला बहन को विमला ने अपनी बात बताई कि वह तो गांधी की राह पकड़ दलित बेटियांे की शिक्षा हेतु काम करना चाहती है। यह भी कि वह राजनीतिक कार्यकर्ता से विवाह नहीं चाहती। कठिन परिस्थिति जान सरला बहन विमला के साथ टिहरी गईं और कांग्रेस कार्यालय में सुन्दरलाल से मिली। सब बातें बता दीं। आजाद भारत के पहले दशक में संभावित राजनैतिक कैरियर को छोड़ समाजसेवा के कठिन मार्ग को थामना सुन्दरलाल का बहुत बड़ा निर्णय था। यह उन दोनों के जीवन में एक नई शुरूआत थी और उत्तराखण्ड में सामाजिक कर्म के क्षेत्र में भी। इसी बीच भिलंगना की उपघाटी बालगंगा के किनारे सिल्यारा में जगह खोजी गई और एक छोटी ठौर जन सहयोग से बनने लगी। यह ‘नवजीवन आश्रम’ इस जोड़े की कर्मस्थली बना। 19 जून 1956 को यहीं ग्रामीणों के बीच विमला और सुन्दरलाल का विवाह हुआ।
अब तक विनोबा का भूदान तथा ग्रामदान का आन्दोलन चल चुका था और विमला देश के अनेक हिस्सों में गई। उत्तराखण्ड के भीतर भी। यदि टिहरी में विमला-सुन्दरलाल ने शुरूआत कर दी थी तो पौड़ी में मानसिंह रावत विदेश अध्ययन की छा़त्रवृत्ति छोड़कर सक्रिय हो गये थे। उधर राधा बहन ने अल्मोड़ा में समाज संगठन का काम संभाल लिया था। 1956 में भूदान के दौरों के समय जी.एम.ओ. के बुकिंग क्लर्क का काम कर रहे चंडी प्रसाद भट्ट पहले मानसिंह फिर जयप्रकाश नारायण के प्रभाव से सर्वोदय कार्य में आ गये। टेलर मास्टरी छोड़ सोहन लाल सर्वोदयी हो गये थे। बहुत सारे और साथी भी विकसित हो रहे थे।
भूदान यात्राओं ने कार्यकर्ताओं को उत्तराखण्ड की आधारभूत समस्याओं को समझने में मदद दी। अगले दशकों में ये मुद्दे आन्दोलनों का विषय बने। शराब, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, जंगल, पानी, महिलाओं और दलितों की स्थिति आदि। देश में अन्यत्र भी वे सभी जा रहे थे। सरला बहन ने विमला को वापस पहाड़ों में बुला लिया। 1960 में तिब्बत से व्यापार बन्द होने के साथ सीमा में तनाव प्रकट हो गया, जिसकी परिणति 1962 का युद्ध था। इन यात्राओं में सीमान्त में दूसरी सैनिक पंक्ति को विकसित करने का प्रयास हो रहा था। कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी टीम विकसित हो गई थी। जय प्रकाश नारायण ने हिमालय सेवा संघ की स्थापना की तो उससे भी ये सभी जुड़े। इस समूह ने श्रमिक सहकारी समितियों का गठन किया। महिलाओं की दयनीय स्थिति और शिक्षा वंचना से यह समूह चिन्तित था। एक से एक आदर्शवादी इसमें थे।
1957 में विमला-सुन्दरलाल की बेटी मधु का जन्म हुआ और 1961 तथा 64 में राजीव तथा प्रदीप का। तीनों बच्चे आश्रम के स्कूल में पढ़े और उनके लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं थी। सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के परिवारों की यही स्थिति थी। बच्चों को शारीरिक श्रम करना पड़ता था। विमला के स्कूल के सभी बच्चे उनके अपने थे और वह अपने जैविक बच्चों की अलग देखरेख नहीं करती थी।
शराबबन्दी: पहला आन्दोलन
घनश्याम शैलानी के शब्दों में ‘शराब के दैत्य’ ने पहाड़ों को बरबाद कर दिया था। सभी भूदान कार्यकर्ता बेचैन थे। उन्हें गांधी के वक्तव्य याद थे और संविधान की धारा 47 भी। 1962 में देहरादून में दर्जी का काम करने वाले सर्वोदयी सोहनलाल भूभिक्षुक ने पहले पोस्टकार्ड अभियान, फिर भट्टियों पर पिकेटिंग और अन्त में लखनऊ विधान सभा की सीढ़ियों पर आमरण अनशन किया। जब विनोबा ने यह कहा कि मरने से नशाबन्दी नहीं होगी तो उन्होंने अनशन वापस ले लिया। पर व्यवस्था की बड़ी झील में पड़े इस कंकर ने लहरें तो पैदा कर ही दीं। सरकार के पास 1962 तथा 1965 के युद्धों को रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने की मंशा थी।
इसी दौर में भिलंगना क्षेत्र में सरकार ने कुछ और तो नहीं किया पर 1965 में घणसाली में शराब की दुकान खोल दी। कहने को प्रदेश सरकार के पास मद्यनिषेध विभाग था पर प्रभुत्व और जलवा आबकारी विभाग का होता था। अंग्रेजों के जमाने से चली जंगलों और शराब की नीलामी अपने को गांधी का उत्तराधिकारी कहने वाली सरकारें हर साल आयोजित करतीं थीं। इस तरह जंगल तथा समाज दोनों की बरबादी होती रही। विकास की पंचवर्षीय योजना को ये दो विनाशकारी सालाना योजनायें लगातार फेल करती रहीं। स्कूल या अस्पताल की तरफ नजर कम जाती थी। ऐसे ही जिन वन पंचायतों की स्थापना शेष कुमाऊ में 40-50 साल पहले अंग्रेजी काल में हो चुकी थी उनको टिहरी जिले में 1959 की बल्देवसिंह आर्य समिति के सुझावों के बाद भी लागू नहीं किया गया।
घणसाली में अप्रैल 1965 में शराब का ट्रक आना था और स्थानीय समाज को विमला-सुन्दरलाल द्वारा प्रतिकार के लिये तैयार किया जा रहा था। रामलीला तथा नाटकों के माध्यम से बात समाज में जा रही थी। सामान्य जन ही नहीं, इलाके के प्रभावशाली लोग भी समर्थन देने आने लगे। कौसानी से सरला बहन अपनी टोली लेकर आ गईं। सुन्दरलाल ने उपवास शुरू किया। अन्यत्र भी आन्दोलन होने लगा। सर्वोदय के कार्यकर्ताओं ने सर्व समर्थन से टिहरी में चम्बा, लम्बगांव तथा चीड़बटिया; चमोली में चन्द्रापुरी; पौड़ी में कोटद्वार तथा सतपुली; पिथौरागढ़ में थल और डीडीहाट तथा अल्मोड़ा में गरुड़ में आन्दोलन चलाया। यह सामाजिक हिस्सेदारी के साथ चला। मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी ने आन्दोलन की बात मानी और 1967 में इन स्थानों पर शराबबंदी हो गई पर इन जिलों में अन्यत्र शराब खुली थी।
1969 में आन्दोलन के दबाव और गांधी जन्म शताब्दी की शर्म से तीनों सीमान्त जिलों-उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़-में शराबबंदी हुई और पौड़ी में टिंचरी के खिलाफ सफल आन्दोलन चला। 1970 में टिहरी और पौड़ी जिले भी नशाबंदी के अन्तर्गत आ गये। आठ में से पांच जिलों में शराबबंदी का लागू होना बहुत बड़ी जीत थी।
इस आन्दोलन में अलग अलग जगहों पर विमला, सुमन की मां तारा देवी, मानसिंह रावत, शशिप्रभा रावत, सोहनलाल भूभिक्षुक, भवानी भाई, घनश्याम शैलानी, सुरेन्द्रदत्त भट्ट, श्यामा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, आनन्द सिंह बिष्ट, राधा बहन, सदन मिश्र, योगेश बहुगुणा, दीवान सिंह भाकुनी, शेर सिंह कार्की आदि कितने ही कार्यकर्ता आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। सबसे उपर सरला बहन और कभी कभी शांतिलाल त्रिवेदी अलग से दिखाई देते थे। कांग्रेस तथा अन्य राजनैतिक पार्टियों के जमीर वाले लोग आन्दोलन को समर्थन दे रहे थे।
अंग्रेजी शराब के कारोबारियों ने उच्च न्यायालय में रिट दायर कर 14 अप्रैल, 1971 को स्टे ले लिया। प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय नहीं गई। फिर आन्दोलन ज्यादा आक्रामकता से चला। सुन्दरलाल ने फिर अनशन शुरू किया। अब चमोली से भी कार्यकर्ता महिलाओं और बच्चों को लेकर टिहरी आये और गिरफ्तार किये गये। बच्चों और महिलाओं सहित आन्दोलनकारियों को सहारनपुर जेल में भेजा गया। घनश्याम शैलानी और चंडी प्रसाद भट्ट पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर लोगों के बीच जाते गिरफ्तार कर लिये गये। दोनों को एक ही हथकड़ी लगाई गई। आन्दोलन के आगे सरकार झुकी।
27 दिसम्बर, 1971 को सरकार ने फिर राजाज्ञा निकाली कि 1 अप्रैल, 1972 से शराबबंदी पूर्ववत लागू कर दी गई है। अगले एक दशक तक सरकार अपने निर्णय पर कायम रही। जब फिर शराब खुली तो 1984 में ‘नशा नहीं रोजगार दो आन्दोलन’ चला, जिसको चिपको आन्दोलन के कारण विश्व विख्यात हो चुके कार्यकर्ता अपना सहयोग नहीं दे पाये। यह विभाजित चिपको का दृश्य था। तबसे नशा सामाजिक रूप से भी सम्मान पाता गया। नया राज्य तो शराब पर निर्भर है। एक बुजुर्ग के शब्दों में इस राज्य की धमनियों में शराब का रक्त बहता है।
चिपको आंदोलन
नशाबंदी आंदोलन ने अनेक कार्यकर्ताओं को उभारा और महिलाओं में गहरा आत्मविश्वास भरा। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी लगा कि महिलाओं की हिस्सेदारी से जनान्दोलन को गरिमा और गहराई साथ साथ मिलती है। जंगलों का मुद्दा दो दशकों से विलम्बित था। आर्य समिति की रपट को आये 10 साल हो चुके थे। छोटी छोटी समितियों के बाद 1970 के आसपास अनेक ग्राम स्वराज्य मण्डलों की स्थापना हुई। इससे सर्वोदय समूह अधिक सुसंगठित हुआ। कुछ आर्थिक क्रियाकलाप और लकड़ी-लीसे और जड़ीबूटी सहित वनोपजों से जुड़े कुटीर उद्योग शुरू हुये।
1970 की अलकनन्दा बाढ़ ने कार्यकर्ताओं और समाज दोनों को यह समझ दी कि यह बाढ़ सिर्फ भूस्खलन, भूकम्प या तालाबों के टूटने से ही नहीं हुई है, इसमें जंगलों के विनाश तथा सड़कों को बनाने के हिमालय विरोधी तरीके का भी योगदान है। राहत कार्य में गये कार्यकर्ताओं ने अपनी आंखों से देखा कि जंगलों के कटान और पेड़ों के लुड़कान ने बाढ़ को प्रलयंकारी बनाने में योगदान दिया था। दूसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा पूर्ववत जारी थी। अब उन काष्ठ प्रजातियों का आवंटन खेल कम्पनियों को किया जाना शुरू हुआ, जो स्थानीय समाज को खेती के उपकरणों के लिये मिलती थीं। स्टार पेपर मिल्स को तो 1958 से ही कौड़ियों के भाव दशकों के लिये जंगल/पेड़ अलाट कर दिये गये थे।
चमोली जिले में 1971 से जगलात आन्दोलन की शुरूआत हुई। अलकनन्दा की बाढ़ से पहला पाठ इसी समाज ने सीखा था। 22 अक्टूबर 1971 को गोपेश्वर में हुआ प्रदर्शन पहली ग्रामीण अभिव्यक्ति थी। 1900 के बाद लगातार चले जंगलात आन्दोलन (‘जंगल सत्याग्रह’) की याद और चेतना अभी समाज मंे थी, जिसे आर्य समिति को इस समाज ने स्पष्ट स्वर में बता दिया था। प्रदर्शनों, प्रतिवेदनों और प्रतिनिधि मण्डलों का सिलसिला चलता रहा। साथ ही मूल भूमि में ग्रामीणों को संगठित करने का काम लगातार जारी रहा।
1972 में पुरौला, उत्तरकाशी तथा गोपेश्वर में क्रमशः प्रदर्शन हुये। साम्यवादी दल उत्तरकाशी में यह सिलसिला पहले शुरू कर चुका था। 15 दिसम्बर 1972 का गोपेश्वर प्रदर्शन ऐतिहासिक था। 27 मार्च 1973 को सायमण्ड कम्पनी के आदमियों का गोपेश्वर आगमन तथा ‘अंगवाल्ठा’ या ‘चिपको’ शब्द की पहली अभिव्यक्ति दशौली ग्राम स्वराज्य मण्डल की सभा में चंडी प्रसाद के मुह से प्रकट हुई। तरह तरह के सुझावों के बाद यह निश्चय ही समाज के अन्तरतम से आई आवाज थी।
इसके बाद 24 अप्रैल 1973 को मण्डल की सभा में चिपको का पहला सार्वजनिक स्वर आलम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में प्रकट हुआ और आवंटित पेड़ों को कम्पनी के आदमी नहीं काट सके। कम्पनी को फाटा में पेड़ दे दिये गये। वहां केदार सिंह रावत के स्थानीय सहयोग से प्रतिकार हुआ और इसमें महिलाओं की प्रभावशाली हिस्सेदारी हुई। सफलता मिली। अब अनेक जंगलों के साथ रेणी का जंगल नीलाम हो चुका था। सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी तथा जन प्रतिनिधि लगातार कार्यरत रहे। भट्ट के साथ गोविन्द सिंह रावत, हयात सिंह सहित अनेक स्थानीय विद्यार्थी थे। गोपेश्वर से जो महिलायें फाटा गईं वे बाद में रेणी भी गईं।
चिपको की चेतना जोशीमठ ब्लाक के अनेक गांवों में टिक सकी। 26 मार्च 1974 को अपने पुरुषों की अनुपस्थिति में (प्रशासन ने चतुराई से इसी दिन भूमि के मुआवजे का भुगतान करने की ठानी) महिलाओं और बेटियों ने गौरादेवी की अगुवाई में अपना मायका बचा लिया। यह घटना विख्यात हुई। पर गौरादेवी चिपको आन्दोलन की जननी नहीं बेटी थीं। जैसे अन्य बेटियां और बेटे थे। इतिहास ने गौरादेवी को एक अलग ऊंचाई दी, जो सर्वथा स्वाभाविक था।
चिपको कमेटी बैठी, उसके सुझाव आये। पर जून 1975 से लगा आपातकाल डेड़ साल तक चिपको के प्रवाह को अवरुद्ध कर गया। कार्यकर्ताओं के मनोविज्ञान में विनोबा और जयप्रकाश में से किसी एक को चुनने का भाव न था। सभी दोनों से प्रेरित रहे थे। आपातकाल के बाद जनता पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षा, नासमझी और गैर जिम्मेदारी ने न सरकार रहने दी, और न जंगलात के मुद्दे सुलझाये जा सके। इस तरह 1977 से 1980 तक चिपको की कितनी ही अभिव्यक्तियों में कार्यकताओं को महिलाओं, विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और हिमालय प्रेमियों का असाधारण समर्थन मिला। मीडिया का भी।
इस क्रम में नैनीताल तथा नरेन्द्रनगर में नीलामियों का सफल विरोध हुआ। गिरफ्तारियां हुईं। फिर अदवाणी, भ्यूंढार, चांचरीधार, बडियारगढ़़, ध्याड़ी, जनोटी पालड़ी, डूगरी पैंतोली, दूधातोली, बछेर और नन्दासैण सहित अनेक स्थानों पर चिपको के विभिन्न रूप प्रकट हुये। ये हिस्सेदारी और सत्याग्रह भाव के हिसाब से अप्रतिम थे। ये सभी चिपको चेतना से जुड़े थे और हरएक अपनी स्वायत्तता भी लिये था। महिलाओं और युवाओं का प्रभुत्व था। नैनीताल, अदवाणी, ध्याड़ी, नरेन्द्र नगर, जनोटी पालड़ी, अलमोड़ा, डूगरी पैंतोली आदि में जबर्दस्त दमन और गिरफ्तारियां हुई। अलमोड़ा जिले में तो कभी कभी एक छापामार लड़ाई का भान होता था। राज्य द्वारा आरोपित हिंसा का प्रतिकार लोगों ने धरनों, नारों, गीतों और गिरफ्तारियों से दिया।
शैलानी, गिर्दा और जीवानन्द श्रियाल जैसे गीतकार चिपको ने दिये थे और धूम सिंह नेगी, गोविन्द सिंह रावत, कमलाराम नौटियाल, शमशेर बिष्ट, बालम जनोटी, बिपिन त्रिपाठी, जसवन्त सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून, प्रताप शिखर, राजीव लोचन साह, पी.सी. तिवारी, सुदेशा, सौपा, नन्दादेवी तथा बचनी देवी, मोहन सिंह, प्रदीप टम्टा सहित दर्जनों कार्यकर्ता-नेता। इस समय दमन का दायरा बढ़ाने वाले उत्तराखण्ड से ही चुने गये दो मंत्री थे। उत्तराखण्ड के समाज को नये प्रतिकारों को विकसित करने से पहले इसे समझना होगा कि चुने जाने बाद हमारे प्रतिनिधि जनविरोधी क्यों हो जाते हैं। क्यों वे जनता द्वारा चुने जाकर भी सिर्फ अपने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि बन कर रह जाते हैं।
उपलब्धियाँ और दरार
हालांकि बहुतों को दिखाई नहीं दे रही थी पर अब तक चिपको में दरार आ चुकी थी। इसमें खुद सर्वोदय के नेताओं का रोल रहा और व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा का भी। 1980 में सरकार बदल जाने के बाद नई सरकार ने सम्वाद किया और निर्णय लिये। सुन्दरलाल यात्राओं और प्रतिनिधि मण्डलों में लगातार चिपको का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने ही रेणी की सफलता के बाद चिपको पर सबसे पहली और बेहतरीन पुस्तिका 1974 में लिखी थी। पर ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से वे अदवाणी तथा बडियारगढ़ में सक्रिय रहे। यह दौर आपात्काल के बाद ही आया। इसलिये सिर्फ किसी एक के लिये ‘चिपको का प्रणेता’ जैसा शब्द इस्तेमाल करने से तनिक बचना उचित होगा। ये तमाम लोग अपने लिये ‘चिपको का कार्यकर्ता’ या ‘संदेश वाहक’ जैसा शब्द इस्तेमाल करते रहे थे।
1980 के वन संरक्षण अधिनियम का लागू होना, 1000 मीटर से उपर हरे पेड़ों के कटान पर रोक लगना और औद्योगिक घरानों को दी गई लम्बी समयावधि और सस्ते दामों वाली लीज का निरस्त होना मामूली बातें नहीं थी। वन मजदूरों की दशा को बदलने और बेहतर बनाने में चिपको का योग रहा। ठेकेदारी प्रथा समाप्त हुई। वन और पर्यावरण का स्वतंत्र मंत्रालय बना। हिमालय को लेकर अनेक कार्यदल बने। वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई। अनेक अन्य पर्यावरण कानून बने। वन आयोग बना और 2006 में वनाधिकार कानून भी आ गया। पर व्यवस्था की भीतरी सड़न कम नहीं हुई। सभी निर्णय लागू नहीं हो सके। कुछ अधूरे मन से, कुछ बस औपचारिक रूप से लागू हुये।
अभी सुन्दरलाल जी को श्रद्धांजलि देने वालों को बांधों और चारधाम सड़कों में नष्ट हुये जंगलों का ख्याल आना चाहिये ? पिछले ही माह जंगलात आन्दोलन द्वारा 1974 में बचाये गये वयाली के जंगल का कोविड जन्य बन्दी के बीच कटान से पसीजना चाहिये? सूखे और छपे पेड़ों के साथ हरे पेड़ भी वहाँ काटे गये। महीपाल, अरण्यरंजन और साहब सिंह अगर वहां नहीं गये होते तो किसी को पता तक नहीं चलता। यह जंगल भागीरथी और उसकी सहायक नदियों के नाजुक जलागम का हिस्सा है। वन निगम ही यह कटान करवा रहा था। वन निगम ने एक मात्र लकड़ी कटान और वितरण का काम कर ठेकेदारी प्रथा को दूसरी तरह से जीवित रखा, इसका भी यह उदाहरण है। इस तरह राज्य जंगलों का संरक्षक नहीं मालिक बना रहा।
अपने नये राज्य में एफ.आर.डी.सी. (वन तथा ग्रामीण विकास आयुक्त) जैसा संयुक्त विभाग बनाया गया। यह शायद आर.एस. टोलिया की दृष्टि थी। पर उसे व्यवस्था टिका नहीं पाई। टोलिया के देहान्त के कुछ ही साल बाद यह व्यवस्था समाप्त कर ली गई। बीस साल की कुछ स्वाभाविक उपलब्धियां हो सकती हैं, जिसे मैं ‘शरमा-शरमी विकास’ कहता हूं, पर ठोस कुछ ज्यादा है नहीं। इतनी शहादतों के बाद मिले राज्य को सबसे ज्यादा नेताओं ने नष्ट किया। नेताओं का इतना पिछड़ापन यह समाज जब तक सहेगा, अभिशप्त रहेगा। पर यह अभी विषयान्तर होगा।
कश्मीर से कोहिमा यात्रा
हर रचनात्मक व्यक्ति बेचैन होता है और सुन्दरलाल भी थे। पिछली फुटकर यात्राओं में हिमालय के कुछ हिस्सों को देख चुके थे। 30 मई, 1981 से किश्तों में सम्पन्न कश्मीर (श्रीनगर) – नागालैंड (कोहिमा) यात्रा 1 फरवरी, 1982 को कोहिमा में समाप्त हुई। लगभग 4800 किमी. लम्बी यात्रा का प्रभाव पता करना मुश्किल हैं। एक मुलाकात में जैसे किसी व्यक्ति को पूरा नहीं जान पाते वैसे ही एक यात्रा में किसी क्षेत्र या विशाल पर्वतमाला को भी गहराई में नहीं जान सकते। दूरस्थ दुर्गम इलाकों में और भी मुश्किल होता है। पर यात्री इन यात्राओं से सदा बहुत सीखते हैं। जैसे उन्हें एक साथ बहुत किताबें पढ़ने का मौका मिला हो।
‘हिमालय बचाओ’ की मूल चेतना इस यात्रा से निकली। यात्री एक साथ पूरे हिमालय को देख रहे थे। अलग अलग देशों, प्रान्तों, पारिस्थितिक खण्डों और अक्षांश-देशान्तरों में बंटा हुआ हिमालय। अलग अलग समुदायों और जीवन पद्धतियों द्वारा संचालित। उसे समझने का यात्रा के अलावा कोई और तरीका भी नहीं था। सुन्दरलाल की हिमालयी दृष्टि इससे बनी। आज हमारे लिये वह एक प्रेरणा की तरह है।
मैंने उनसे शायद 1995-96 में पूछा था कि लिखेंगे कब अपने अनुभवों को ? उनका मुस्कान के साथ उत्तर था कि आपने (वह तुमने नहीं बोलते थे) तीन अस्कोट आराकोट यात्रायें कर डाली हैं पूरी की पूरी, तो क्यों नहीं लिखा? मैं निरुत्तर था। फिर कहा कि लिखने का समय भी आयेगा। हिमालय की विशालता और इतनी तरह की विविधता को अभी और समझना है। पूर्व में अलग, मध्य में अलग और पश्चिम में अलग। समस्याएं और चुनौतियां एक तरह की। सम्पदा की लूट और पिछड़ापन या मासूमियत एक तरह की। मैं सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। इसी तरह की बात चंडी प्रसाद भट्ट या राधा बहन भी करती रहीं जब उनसे यात्राओं पर कुछ लिखने का आग्रह किया जाता।
टिहरी बांध विरोधी आन्दोलन
बहुतों को याद नहीं होगा कि टिहरी क्षेत्र से भारत की पहली संसद में सदस्य रही कमलेन्दुमती शाह ने 1969 में टिहरी बांध के विरोध में पत्र भेजा था। ‘गढ़वाली’ के सम्पादक विश्वम्भर दत्त चंदोला ने कभी इसी तरह के विचार रखे थे। टिहरी जिला परिषद ने 1972 में सर्वसम्मत प्रस्ताव बांध के विरोध में सरकार और जन प्रतिनिधियों को भेजा था। टिहरी की महानतम हस्ती, संग्रामी और वकील वीरेन्द्र दत्त सकलानी (जो ग्राम सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक भी रहे थे) ने टिहरी बांध के तमाम आयामों पर विस्तृत अध्ययन कर और इस हेतु टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति बनाकर 1978 में सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदन किया था। सकलानी के अध्ययन और भावना का सार था कि ‘टिहरी बांध सम्पूर्ण विनाश का प्रतीक है’।
1 जून 1978 को जब काम शुरू हुआ तो लोगों ने बांध स्थल पर धरना दिया था। बहुगुणा इस आन्दोलन में प्रत्यक्ष 1985 में आये जब वे कुछ फुरसत पा गये थे। पर वे प्रारम्भ से ही इसके विरोध में थे और मनेरी-भाली जैसी छोटी परियोजना के पक्ष में ‘धर्मयुग’ में लेख भी लिख रहे थे। छोटी परियोजनाओं के औचित्य पर उन्होंने ‘धार ऐंच पाणि ढाळ पर डाला, बिजली बणावा खाळा-खाळा’ अर्थात ‘पहाड़ की चोटी पर पानी, ढलानों पर पेड़ और गाड़-गधेरों में बिजली’ का सूत्र दिया था।
भागीरथी और भिलंगना घाटियों की सिर्फ कृतघ्न संतानें ही बांध का पक्ष ले सकती थीं। अतः लगातार जन समर्थन मिला। 1989 में सकलानी के अधिक अस्वस्थ हो जाने के बाद कमान सुन्दरलाल ने संभाली। 24 नवम्बर 1989 को उन्होंने टिहरी में घोषणा की कि जब तक टिहरी बांध परियोजना रद्द नहीं होगी वे सिल्यारा नहीं जायेंगे। वे नहीं गये, नहीं जा सके। तीन दशक तक अपने घर न जा पाने का दर्द अपार था। मध्यप्रदेश की छोटी कस्सारट में ऐसी ही जिद बाबा आमटे ने भी की। नर्मदा में बन रहे बांधों के खिलाफ। पर अन्त में उनको स्वास्थ्य के कारणों से जाना पड़ा। सुन्दरलाल टस से मस नहीं हुये। 1991 के भूकम्प के समय विमला भूकम्प से ध्वस्त सिल्यारा गईं। हमारी उनसे तब वहीं मुलाकात हुई थी।
टिहरी की जनता, वहां के बहुत से सामाजिक-राजनैतिक कार्यकर्ताओं और विमला-सुन्दरलाल के जीवन का एक बड़ा अनुभव रहा टिहरी बंाध विरोधी आन्दोलन। यह हार की जीत थी। भारत सरकार जिन वास्तविकताओं को स्वीकारती थी, उनकी ही अवमानना करती थी। वैज्ञानिक कमेटियां बिठाई पर बात उनकी नहीं मानी। विनोद गौड़ तथा जेम्स ब्रून के आर.आइ.एस. फैक्टर को स्वीकारा पर लागू नहीं किया। 1990 में डी.आर. भुम्बला की अध्यक्षता वाली समिति ने छोटे बांधों का सुझाव दिया। कौन मानता ? हनुमन्ता राव की बातें सराही गईं पर मानी नहीं गई। 20 अक्टूबर, 1991 के 6.6 रैक्टर के भूकम्प से भी सरकार ने नहीं सीखा।
दूसरी तरफ स्थानीय समाज को भ्रष्ट किया गया। नकली मकान बनाने और उनके मुआवजे की व्यवस्था कर दी गई। स्थानीय समाज विभाजित होता गया। अनेक पत्रकार और नेता खरीदे जा चुके थे। निहित स्वार्थ इतने सुसंगठित पहले कभी नहीं दिखे। एक ऐतिहासिक शहर, दो घाटियों में फैले सम्पन्न खेतीहर समाज को नियोजित तरीके से उजाड़ा गया। अब टिहरी झील की सतह पर मोटरबोट में सैर कराने या करने वाले जो डूब गया उसका अर्थ कभी समझेंगे क्या? उन्हें तो प्रतापनगर की ओर के धंसते पहाड़ या पानी की सतह के अनुसार बदलते मुर्दाघाट भी नजर नहीं आयेंगे।
बांध विरोधी आन्दोलन में सुन्दरलाल ने कम से कम चार बार अनशन कर अपने प्राणों को जोखिम में डाला। उनका शरीर अनशनों के दुष्प्रभाव को अंत तक झेलता रहा। धीरे धीरे साथी कम होते गये। यह उनकी नहीं, उस समाज की पराजय थी, जो पिछली डेढ़ सदी से अपने गांवों से भाग रहा था। उस समाज का मनोविज्ञान नर्मदा के किसानों की तरह का नहीं था, जो नाउम्मीदी के बावजूद अभी भी लड़ रहे हंै। पर टिहरी की हार इस अर्थ में जीत थी कि देश के अधिकांश लोगों ने यह महसूस किया कि टिहरी में गलत किया जा रहा है। आन्दोलन ने जरूर पुनर्वास में कुछ मदद की। नर्मदा आन्दोलन ने भारतीय राज्य की नग्नता पूरी दुनियां के सामने रख दी। नये क्षेत्र में तथाकथित सिंचाई व्यवस्था करने के लिये एक प्राचीनतम खेतिहर-पशुचारक समाज को समयबद्ध तरीके से उजाड़ा गया।
टिहरी आन्दोलन के बाद न सुन्दरलाल सिल्यारा लौट सके न विमला। ‘गंगा हिमालय कुटी’ में डूबती टिहरी के अंतिम गवाह के रूप में इन दोनों को देखना उदास करता था पर आशाहीन नहीं, क्योंकि उनके तर्क सही थे। सिल्यारा आश्रम तीस से अधिक सालों से अपने संस्थापकों का इन्तजार करता रहा है। विमला का तो शिक्षा और संगठन का अपना ऐजेण्डा ही स्थगित हो गया। पर वे सुन्दरलाल के साथ छाया नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानव व्यक्तित्व और आन्दोलनकारी की तरह रहीं। वे अपने जीवन साथी की जिद जानतीं थीं और उनके भीतर छिपी वह बेचैनी भी जो अपनी धरती उजड़ने देने को तैयार नहीं थी। सुन्दरलाल की ऊँचाई बिना विमला के नहीं बनती है, इसे नहीं भूलना चाहिये।
हिमालय बचाओ
कश्मीर कोहिमा के सघन अनुभवों और टिहरी आन्दोलन की जीत न हो सकने के बाद सुन्दरलाल को लगा कि हिमालयी विकास की कोई वैकल्पिक दृष्टि और नीति होनी चाहिये। ‘हिमालय बचाओ’ की चेतना इस यात्रा से और टिहरी के अनुभवों से निकली। हिमालय में यु़द्धजन्य परिस्थिति से शुरू हुआ ‘विकास’ बाद में बाजार की अर्थव्यवस्था, भोगवाद, कारपोरेट वर्चस्व के दौर में ‘महाविकास’ में बदल गया। भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह हिंसा और विध्वंस से भरपूर हो गया। इसने तीर्थयात्रा को फूहड़ पर्यटन में बदलने का दुस्साहस किया। 1991 का भूकम्प, 2013 की महाआपदा और अब 2020-21 की महामारी से भी जो व्यवस्था विवेक और सही रास्ता अर्जित नहीं कर सकी, वह जन आन्दोलन या सुन्दरलाल के कहने से मान जायेगी यह सोचना कहीं से भी सही नहीं होगा। पर यह समाज और इसके सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता चुप हो जांय, यह अपेक्षा भी मान्य नहीं हो सकती।
‘हिमालय बचाओ’ का दस्तावेज अधूरा रहा। क्योंकि इसको संस्कृति कर्मियों, वैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकांे का अधिक तार्किक आधार नहीं मिला। इसे अधिक लोगों के बीच नहीं ले जाया जा सका। हमारे पास ऐसे विज्ञानी थे नहीं जो अपने सीमित अनुशासनों या विशेषज्ञता से बाहर निकल सके हों। पत्रकार-लेखकों की रचनात्मक टोली भी नहीं बनी। जबकि छोटे से देश भूटान ने अपने देश में विकसित ‘सकल राष्ट्रीय खुशी’ (जी.एन.एच.) के दर्शन पर बहुत अच्छी चर्चा करके उसे परोसने और स्वीकार करने लायक बना दिया है।
‘पारिस्थितिक समाज’ का विचार विकसित होना कठिन तो है पर जरूरी भी। पूंजी कभी भी पारिस्थितिकी को नहीं बख्शती है और न तकनीक ही हर बार समता की ओर ले जा सकी है। पारिस्थितिक समाज का विचार परम्परा में सदा निहित रहा पर परम्परा में मामूली और गैर जरूरी चीजें भी कम नहीं थीं। माक्र्स-ऐंगिल्स के ‘डायलैक्टिक्स ऑफ नेचर’ या गांधी के ‘हिन्द स्वराज’ में इसके वैचारिक बीज खोजे जा सकते हैं। उनके बाद के तमाम और लोगों में इस जरूरी विचार के सूत्र या परछाइयां पाई जा सकती हैं। सरला बहन ने भी यह कोशिश की थी। जिस समाज में तीन चैथाई से अधिक जनसंख्या दयनीय हालत में हो और मुट्ठी भर लोग देश की प्राकृतिक सम्पदा, सम्पत्ति और समृद्धि पर कब्जा किये हों; मध्यम वर्ग जहां सिर्फ अपनी धुन में रहता हो; चिंतकों के स्थान पर जहां चाटुकार प्रभावी हों; मीडिया जहां मृतप्राय हो वहां ‘पारिस्थितिक समाज’ का विचार जन-गण के मन तक कैसे जाय यह बहुत बड़ा सवाल है। इसकी अपेक्षा सिर्फ सुन्दरलाल से करना उचित नहीं है।
इसलिये कभी भी हिमालय को क्यों, किससे और कैसे बचाना चाहिये का गहन विश्लेषण नहीं हो सका। इस बड़ी बात को बहुत से छोटे मुह वाले ठीक से कह भी नहीं पाते थे। सत्ता से सम्वाद तो शायद करना पड़ेगा पर सत्ता से सम्मान लेकर यह कठिन विचार विकसित नहीं हो सकता है। जिन सरकारी सम्मानों को सरला बहन ने खारिज कर दिया था आज उनके आधार पर हम सुन्दरलाल को तोलते हैं। क्या इनके बिना वे छोटे होते? कोई सज्जन कह रहा था कि उनको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिये। क्यों नहीं ! हिमालय चेतना बनाने के लिये दिया जाना चाहिये। पर सोचिये जरा कि दलाई लामा को नोबल पुरस्कार मिलने से तिब्बत का प्रश्न कहीं से सुलझता हुआ लगा? कैलाश सत्यार्थी को नोबल मिल जाने से बंधुवा बच्चों और भारतीय बचपन की दिक्कतें सुलझ गईं? व्यक्तिगत शोमा कभी सामाजिक सौन्दर्य का सृजन नहीं करती हैं।
एक और बात सामने आती है। शार्ट कट के कारण अनेक बार सामाजिक कार्यकर्ता अपनी छबि धूमिल कर जाते हैं। मई 1973 में सुन्दरलाल गोपेश्वर आकर पैदल यात्रा में निकल गये जबकि फाटा आन्दोलन की तैयारी हो रही थी। चिपको आन्दोलन में 1976-79 का समय ऐसा रहा जब चिपको पर कुछ ऐसे लिखने वाले आये जिन्होंने झूठ लिखा और आन्दोलन के मुख्य लोगों के बीच कभी न पटने वाली दरार डाल दी। जब सुन्दरलाल को अन्त में ‘इकोलाजी इज परमानेंट इकोनॉमी’ ही कहना था तो उन्होंने उस झूठ को क्यों प्रचारित होने दिया कि चमोली में चिपको आर्थिक था और अदवाणी में वह पारिस्थितिक हो गया। चंडीप्रसाद को वे अपना नेता कहते थे। फिर यह मतिभ्रम क्यों हुआ?
इसी तरह बी.बी.सी. को चिपको के नाम पर स्वयं पर केन्द्रित फिल्म बनाने से मना न करना भी चूक कही जायेगी। तभी से चिपको आन्दोलन की नकली फोटो चल पड़ी, जिन्हें सबसे पहले जयन्तो बन्द्योपाध्याय ने पकड़ा था। प्रत्यक्ष आन्दोलन में कभी कोई कैमरा लेकर नहीं गया था। यह राज्यपाल की उपस्थिति में वन महोत्सव नहीं था। ग्रामीण जन अपनी अस्तित्व रक्षा के लिये आये थे। चिपको आन्दोलन में एक घटना छोड़कर कभी चिपकने की नौबत नहीं आई। यह नारा ही काफी था। एक बार पेड़ से चिपकना धूमसिंह नेगी के हिस्से आया। सर्वोदय के प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय नेताओं ने भी गलतफहमियों में कम योगदान नहीं दिया। पर जिन कमजोरियों का फायदा उठाया गया वह तो यहां के आन्दोलनकारियों की थीं।
टिहरी बांध आन्दोलन के समय वे विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं के बहकावे में आ गये। जो फिर कभी गंगा के पक्ष में नजर नहीं आये। इसी तरह उपवास, भूख हड़ताल या अनशन वाला पक्ष भी व्यक्तिवादी लगता है। यह दरअसल उनकी कमजोरी थी पर वे इसे ब्रह्मास्त्र समझते थे। विनोबा ने ही नहीं, सरला बहन ने भी इसकी साफ मनाही की थी। कहा था कि जब जन सहयोग मिल रहा हो, साथी सक्रिय हों तो अनशन क्यों किया जाय। इससे आन्दोलन व्यक्ति केन्द्रित हो जाता था। उनके कुल सात या आठ उपवास चर्चित रहे। दो बार नशाबन्दी में, दो बार चिपको आंदोलन में और चार बार टिहरी बांध आंदोलन में। उनको आजादी से पहले एक बार और आजादी के बाद अनेक बार जेल जाना पड़ा।
23 जून, 1995 को तो उन्हें 70 से भी अधिक दिन उपवास करते हो गये थे। यह लगभग दर्शनसिंह फेरूमान का चण्डीगढ़ को पंजाब को देने के लिये की गयी भूख हड़ताल की तरह था। हर बार कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आश्वासन देता और लगता कि शायद अब बांध का काम रुक जायेगा। पर यह भ्रम में रखना ही था। क्योंकि फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। वे भी यह भूल जाते कि वे सामाजिक आन्दोलनकारी हैं, राजनैतिक आन्दोलनकारी नहीं। उनकी सीमा सत्याग्रह है, जिसका सम्मान सरकारें नहीं करतीं हैं। जरा सोचें कि चारधाम सड़कों या पंचेश्वर बांध के खिलाफ आज वे या कोई भी आन्दोलन कर सकते थे? प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल को किस तरह सरकार ने मृत्यु शैया से बाहर नहीं निकलने दिया, जबकि उनकी मांग टिहरी बांध के मुकाबले सामान्य थी।
जोड़ने वाले
अगर उक्त तमाम जन आन्दोलनों को सामूहिकता और बड़ी टीम से जोड़ दें, विभिन्न विचारों के कर्मठ और सम्वेदनशील लोगों के सहयोग को भी स्वीकार करें तो भी हिमालयी चेतना को फैलाने में उनका योग प्रतीकात्मक रूप से भी कम नहीं है। एक सक्रिय पत्रकार और प्रान्जल गद्य लेखक के रूप में वे सदा याद किये जायेंगे। ‘बागी टिहरी’, ‘उत्तराखण्ड में एक सौ बीस दिन’, ‘धरती की पुकार’, तमाम चिपको पुस्तिकायें और पिछले 50-60 साल के दौर में लिखे गये लेख उनके योगदान को उजागर करने के साथ हमारे समाज के लिये भी उपयोगी होंगे। उनकी अपनी विकास यात्रा के संदर्भ भी हैं।
वे एक जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में भी याद किये जायेंगे। यह बड़े ‘सामाजिक स्वार्थ’ से जुड़ा हुआ था। वे चाहते थे कि विचारवान, रचनात्मक और सृजनशील लोग आपस में जुड़ें। अनेक बार तो वे एक सी वृत्ति या रुझान के लोगों को मिलाते तो कभी अलग अलग तरह के लोगों को, जो बाद में फिर मित्र या सहयात्री हो जाते। जनवरी 1974 में एक अन्जान विद्यार्थी का ‘शक्ति’ पत्रिका में छपा लेख पढ़ कर वे उसे खोजने निकल गये। अन्ततः उन्होंने शमशेर और मेरी मुलाकात कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर से कराई और अस्कोट-आराकोट अभियान का विचार हमारे दिमाग में बो दिया। इसी तरह प्रभात उप्रेती, भगवती नौटियाल की टीमों को जोड़ने का काम था या कुल भूषण उपमन्यु और पाण्डुरंग हेगड़े को। और भी कितने ही। ये सभी हमारे हीरे बने।
किसी भी शहर में जाने पर वे प्रबुद्ध लोगों से मिलते। शायद 1976-77 की बात है। मैं कोटद्वार में भैरव दत्त धूलिया के पास ‘कर्मभूमि’ की फाइलें देख रहा था। बाहर खुली छत पर उनके साथ मुकुन्दीलाल, चन्द्रसिंह गढ़वाली, बनारसीदास चतुर्वेदी बैठे थे। कुछ देर बाद शिवप्रसाद डबराल के साथ सुन्दरलाल बहुगुणा आते हुये दिखे। दरअसल सुन्दरलाल दोगडा में डबराल से मिलकर उन्हें बनारसीदास चतुर्वेदी से मिलाने कोटद्वार लाये थे। वे उन्हें ‘कर्मभूमि’ के दफ्तर में ले आये। इतनी प्रतिभाओं को एक साथ देखना मेरे लिये दुर्लभ अनुभव था। एक बार वे नैनीताल आये मुझे उनको लेकर डी.डी. पन्त, के.एस. वल्दिया, प्रताप भैया, चन्द्रलाल साह और शुकदेव पांडे के यहां जाना पड़ा। फिर वे आनन्द निवास में गंगा बहन से मिल कर राजीव लोचन साह के पास गये। ऐसा वे हर कहीं करते थे।
विमला और सुन्दरलाल
1956 के बाद हम सुन्दरलाल के एक व्यक्ति और सामाजिक चिन्ताओं के लिये जूझने का हुनर प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता के रूप में विकसित होने में विमला का योगदान नहीं भूल सकते। वे छाया की तरह नहीं सम्पूर्ण कार्यकर्ता की तरह उनके साथ थीं। इससे सुन्दरलाल की ऊँचाई बढ़ती जाती थी। 1990 के बाद विमला को अपना कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। नवजीवन आश्रम श्रीहीन हो गया। कोई और कार्यकर्ता वहां नहीं टिक सका। सर्वोदयी संस्थाओं को पर्याप्त खुला और सार्वजनिक नहीं बनाया जा सका। इसलिये एक एक कर ये जीवन्त स्थान जीवन शून्य हो रहे हैं। कुछ में तो कब्जे भी हो गये हैं या उजड़ गये हैं। जैसे शेरसिंह कार्की का मवानी आश्रम या सदन मिश्रा की मेहनत से बना उडियारी आश्रम।
पर लगभग तीन दशक से ज्यादा समय तक नवजीवन आश्रम सिल्यारा ने इस क्षेत्र की चेतना बढ़ाने में बहुत बड़ा योग दिया। इसके बिना हमें चन्द्र सिंह जैसे अधिकारी, बिहारीलाल जैसे समाजकर्मी, त्रेपन सिंह चैहान जैसे कार्यकर्ता और लेखक, भगवती प्रसाद मैठाणी जैसे भूगोलविद, वाचस्पति मैठाणी जैसे संस्कृतज्ञ या भगवती नौटियाल जैसे जंगलात तथा लोक हुनरों के विशेषज्ञ नहीं मिलते। इसी तरह की भूमिका टिहरी के ठक्कर बापा छात्रावास की भी रही।
सुन्दरलाल की महिलाओं के प्रति अधिक जिम्मेदारी का भाव निश्चय ही विमला से अनुप्रेरित था। दलितों के पक्ष में लड़ने का सूत्र उन्हें गांधी से मिला था पर महिलाओं के प्रश्नों, उनकी सामाजिक स्थिति और पुरुष नेतृत्व की सीमित दृष्टि पर उनकी नजर विमला के संग आने के बाद ही गई। शायद सरला बहन को उन्होंने तभी ज्यादा समझा। वे अनेक बार कहते रहे कि जब तक आधा समाज पीछे और वंचित रहेगा तब तक सामाजिक लड़ाइयों का औचित्य कायम रहेगा।
कहा जाता है कि कमियां गांधी में भी थी, तो सुन्दरलाल उनसे मुक्त कैसे हो सकते थे। पर सामाजिक कर्म में इतिहास किसी को गल्तियां सुधारने का मौका नहीं देता है। हिमालय चेतना बनाने, हिमालय के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, पानी के संकट, विस्थापन और पलायन के सवालों को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर निरंतर उठाने के लिये वे याद किये जाते रहेंगे। वे एन.जी.ओ. युग से पहले के स्वयंसेवी थे। अपने पर न्यूनतम खर्च करने वाले। 80 साल की उम्र में वे बस यात्रा कर रहे थे। अब ऐसे 2-4 ही बचे हैं। वे जिद्दी थे। शायद जिद कर्मठता का हिस्सा भी है पर सामाजिक आन्दोलनों तथा परिवर्तन के लिये एक न्यूनतम लचीलेपन की भी जरूरत होती है। उत्तराखण्ड की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान सबसे ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक आन्दोलनों से ही बनी। इसमें सुन्दरलाल बहुगुणा की महत्वपूर्ण भूमिका सदा याद की जायेगी।

पहाड़ के संपादक व संस्थापक शेखर पाठक प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक हैं। वे कुमाऊँ विश्वविध्यालय में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। वे नेहरू मेमोरियल म्यूज़ीयम, नई दिल्ली व इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के फ़ेलो भी रहे हैं। पहाड़ों के गहन जानकार, उन्होंने पहाड़ों को समझने से लिए कई यात्राएँ की एयर लगभग सभी असकोट आरकोट यात्राओं में भागीदारी की।